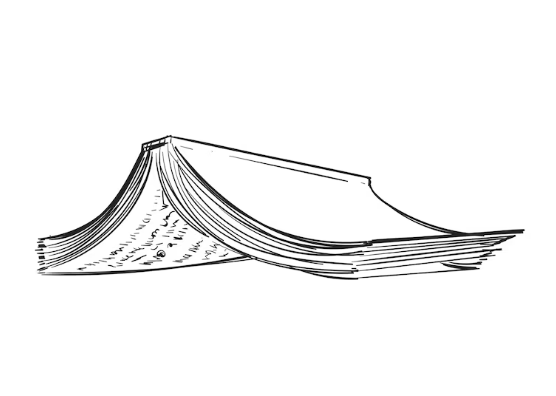लघु पत्रिका (लिटिल मैगजीन) आन्दोलन मुख्य रूप से पश्चिम में प्रतिरोध (प्रोटेस्ट) के औजार के रूप में शुरू हुआ था। यह फ्रांस के रेसिस्टेंस ग्रुप से प्रेरित था। यह प्रतिरोध राज्य सत्ता, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद या धार्मिक वर्चस्ववाद – किसी के भी विरुद्ध हो सकता था। लिटिल मैगजीन आन्दोलन की विशेषता उससे जुडे़ लोगों की प्रतिबद्धता तथा सीमित आर्थिक संसाधनों में तलाशी जा सकती थी। अक्सर बिना किसी बडे औद्योगिक घराने की मदद लिये, किसी व्यक्तिगत अथवा छोटे सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप निकलने वाली ये पत्रिकायें अपने समय के महत्वपूर्ण लेखकों को छापतीं रहीं हैं।
भारत में भी सामाजिक चेतना के बढने के साथ-साथ बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लघु पत्रिकायें प्रारम्भ हुयीं। 1950 से लेकर 1980 तक का दौर हिन्दी की लघु पत्रिकाओं के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यह वह दौर था जब नई- नई मिली आजादी से मोह भंग शुरू हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में लोग विश्वास करने लगे थे कि बेहतर समाज बनाने में साहित्य की निर्णायक भूमिका हो सकती है।
यूं तो हिंदी में साहित्यिक पत्रिकाओं का लंबा और समृद्घ इतिहास रहा है लेकिन हर साहित्यिक पत्रिका लघुपत्रिका नहीं कही जा सकती। आज के समय में मुख्यधारा की पत्रिकाएं व अखबार, कारपोरेट जगत व सम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव में समाहित हो रहे हैं। इस वजह से देश के चौथे स्तंभ के प्रति पाठकों में संशय उत्पन्न होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में लघु पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लघुपत्रिकाएं पिछलग्गू विमर्श का मंच नहीं हैं। लघु पत्रिका का चरित्र सत्ता के चरित्र से भिन्न होता है, ये पत्रिकाएं मौलिक सृजन का मंच हैं।
दरअसल हिंदी में लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत छठे दशक में व्यवसायिक पत्रिका के जवाब के रूप में की गई। इस आंदोलन का श्रेय हम हिंदी के वरिष्ठ कवि विष्णुचंद्र शर्मा को दे सकते हैं। उन्होंने 1957 में बनारस से ‘कवि’ का संपादन-प्रकाशन शुरू किया था। कालांतर में और भी कई लघु पत्रिकाएं व्यक्तिगत प्रयासों और प्रकाशन संस्थानों से निकली, जिसने हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उसका विकास भी किया। बेनेट कोलमैन & कम्पनी तथा हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड की पत्रिकाओं-धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, सारिका, कादम्बनी, दिनमान, और माधुरी जैसी बडी पूंजी से निकलने वाली पत्रिकाओं के मुकाबले अणिमा, कहानी, नई कहानियां, कल्पना, लहर, वातायन, बिन्दु, क्यों, तटस्थ, वाम, उत्तरार्ध, आरम्भ, ध्वज भंग, सिर्फ, हाथ, कथा, आलोचना, कृति, क ख ग, माध्यम, वसुधा ऐसी पत्रिकाएं, बडे प्रतिष्ठानों से नहीं, बल्कि लेखकों के व्यक्तिगत, निजी प्रयत्नों से छोटे पैमाने पर निकलीं। उस वक़्त ऐसी पत्रिकाओं की जैसे झड़ी ही लग गई: समझ, आवेग, सनीचर, अकविता, पहल, आकंठ, इबारत, जारी, ज़मीन, आइना, कंक, अब, आमुख, तेवर, धरातल, आवेश, आवेग, धरती, वयं, संबोधन, संप्रेषण जैसी पत्रिकायें निकलीं जो सीमित संसाधनों, व्यक्तिगत प्रयासों या लेखक संगठनों की देन थीं. इन पत्रिकाओं का मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोध था और ये शोषण, धार्मिक कठमुल्लापन, लैंगिक असमानता, जैसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध खड़ी दिखायीं देतीं थीं।
एक समय तो ऐसा भी आया जब मुख्य धारा के बहुत से लेखकों ने पारिश्रमिक का मोह छोड़कर बडी पत्रिकाओं के लिये लिखना बन्द कर दिया और वे केवल इन लघु पत्रिकाओं के लिये ही लिखते रहे। बडे घरानों की पत्रिकाओं में छपना शर्म की बात समझा जाता था और लघु पत्रिकाओं में छपने का मतलब साहित्यिक समाज की स्वीकृति की गारंटी होता था। इन्होंने रचनाशीलता का एक अलग ही माहौल बनाया। इनमें से ज़्यादातर में दृष्टि थी, रचना-विवेक था और इन्हें लेखकों का अकुण्ठित सहयोग प्राप्त था। लघु पत्रिकाएं घटनाओं की जड़ तक पहुंचकर सच्चाई को उजागर करने का काम कर रही थीं। इनसे एक ओर जहां नवलेखन पल्लवित होता है, वहीं सामान्यजन की आशा-आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। लोग पारिश्रमिक देने वाली और लेखक को स्टार बनाने वाली पत्रिकाओं में छपने की जगह इनमें छपना गौरव की बात समझते थे।
सारी बड़ी बहसें इन्हीं छोटी पत्रिकाओं में चली हैं। आज जो भी लिखा जा रहा है उसके प्रकाशन का मंच यही पत्रिकाएं हैं लेकिन इन लघु-पत्रिकाओं की सीमा भी है।
-प्रसार बहुत कम। (वैसे, अगर संतोष करना चाहें तो यह तथ्य कि टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेण्ट और न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स की बी 7-8 हज़ार प्रतियां ही छपती हैं)।
-सम्पादकीय दृष्टि का अभाव
-रचनाओं का अभाव
-सम्पादक की महत्वाकांक्षा
-व्यवसायिक/आर्थिक विवशताएं
एक कम संसाधनों वाली अच्छी साहित्यिक-वैचारिक लघुपत्रिका निकालना बेहद कठिन काम है। एक तो अच्छी सामग्री जुटाना, बार बार उन्हीं चलताऊ घिसे-पिटे नामों से इतर अपने कर्म के प्रति गंभीर एवं नए रचनाकारों से जनपक्षीय तथा वैज्ञानिक दृष्टिसंपन्न रचनाएं एकत्रित करना एक श्रमसाध्य और गंभीर काम होता है। इसमें एक सुस्पष्ट, संतुलित और चेतस संपादकीय दृष्टि का होना आवश्यक होता है। ढेरों सामान्य, एकरस, बड़े नामों को बॉंड बनाकर भुनाने वाली, विज्ञापनों से धन बटोरने वाली, सरकारी कृपा पर निर्भर रहनेवाली, एक समूह के हितों को संपुष्ट करने वाली यशकामी-महत्वाकांक्षी अवसरवादी संपादकों की व्यक्तिगत कुंठाओं को ढोने वाली, सजावटी शो रूम पत्रिकाओं की भीड़ में निस्पृह रहकर पत्रिका निकाल पाना एक स्वप्न जैसा ही लगता है। क्या ऐसा संभव है? बीसवीं सदी के प्रारंभ में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसे अनेक मूल्यवान सार्थक प्रयास हुए। बीसवें दशक के उत्तरार्ध में भी कई पत्रिकाएं इस कसौटी पर खरी उतरीं। लघुपत्रिका आंदोलन का एक प्रभाव रहा लेकिन आज वह दृष्टि, लगन, समर्पण और ‘स्व’ से विलग होने का भाव कम ही दिखाई देता ह। ऐसे प्रयासों में लोगों का सहयोग भी अत्यल्प होता है| क्या ऐसे प्रयास सफल हो सकते हैं? जन सहयोग अगर हो तो अवश्य ही यह संभव है।
आज राष्ट्रीय एवं ग्लोबल कारणों से न तो लघु-पत्रिकाएं निकालने वालों के मन में पुराना जोश बाकी है और न ही उनमें छपना पहले जैसी विशिष्टता का अहसास कराता है। फिर भी लघु पत्रिकाओं में छपी सामग्री का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है।
हिन्दी साहित्य के बहुत सारे विवाद, आन्दोलन, प्रवृत्तियों को निर्धारित करने वाली सामग्री और महान रचनायें इन लघु- पत्रिकाओं के पुराने अंकों में समाई हुई हैं। इनमें से बहुत सारी सामग्री कभी पुनर्मुद्रित नहीं हुई। साहित्य के गंभीर पाठकों एवं शोधार्थियों के लिये इनका ऐतिहासिक महत्व है। आज का समय बहुत जटिलता लिये हुए है, यह सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संक्रमण का समय है। अब भी इस डिजिटल और सोशल मीडिया वाले दौर में कुछ लघु पत्रिकाएं हैं जो सामाजिक व राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए साहित्यिक चेतना जगाने का काम कर रही हैं। यह सुखद है।
मई 2022 में समकालीन जनमत पत्रिका में साथी कौशल किशोर का लघुपत्रिकाओं पर एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका एक अंश उद्धृत करना प्रासंगिक लग रहा है। वह कहते हैं- यह समय है जब लघु पत्रिकाओं में भी बदलाव दिखता है। वाम-जनवादी दिशा और तेवर की जगह अस्मिता विमर्श, सांप्रदायिकता का सवाल, उपभोक्तावाद, बाजारवाद आदि लेता है। विचार की जगह बाजार प्रधानता ग्रहण करता है। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कारों आदि की ऐसी नकली होड़ शुरू हुई जिसने मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा, व्यक्तिवाद, अवसरवाद जैसी पराई प्रवृत्तियों को बढ़ाने का काम किया। वस्तुपरकता का पहलू कमजोर हुआ। रचनाकारों में आत्मपरकता, आत्मश्लाघा, आत्मप्रशंसा, आत्मप्रचार बढ़ा। इस दौर की अधिकांश पत्रिकाएं व्यक्तिगत प्रयासों से निकली हैं/निकल रही हैं। सामूहिकता की भावना यानी जनवाद का पक्ष कमजोर हुआ है। ऐसे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार आवश्यक है –
1. स्वतंत्र रूप से निकलने वाली पत्रिकाओं तथा सरकारी संस्थानों-अकादमियों से जो निकलती है, इनमें क्या कोई विशेष अंतर है? अगर नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?
2. साहित्यिक पत्रिकाओं के चरित्र को देखें। जहां कुछ के पास संसाधनों का घोर अभाव है। उनके लिए एक-एक अंक के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। कहीं न कहीं उनका कमिटमेंट और जुनून है, जिसकी वजह से पत्रिकाएं निकलती हैं। वहीं, कुछ के पास संसाधनों और विज्ञापनों की कोई कमी नहीं। वह कलेवर में साहित्यिक दिखती हैं लेकिन संचालन में व्यवसायिक हैं। बहुत कुछ इनका नजरिया बकौल धूमिल ‘विरोध में हाथ भी उठा रहे और कांख भी ढ़की रहे’ रहता है। ऐसी पत्रिकाओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या हो ?
3. क्या आज की पत्रिकाओं का एक ही चेहरा है? उनके बीच क्या फर्क है या किया जाना चाहिए? इनके बीच क्या कोई विभाजन रेखा है?
4. साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के स्वरूप व चरित्र में आए बदलाव को देखते हुए क्या वर्तमान में उन्हें ‘लघु’ नाम देना उचित है ? लघु से हमारा आशय क्या है ? इनकी प्रतिबद्धता क्या हो ?
‘प्रेरणा अंशु’ ने दिनेशपुर (रुद्रपुर, उत्तराखंड) में 8 व 9 मई को दो दिनों का लघु पत्रिका सम्मेलन का आयोजन किया। यहां हुई बहस काफी जीवन्त और व्यवहारिक रही। लोगों ने पत्रिका प्रकाशन के अपने अनुभव को साझा किया। अब तक चार लघु पत्रिका सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला सम्मेलन 2001 में हुआ था। दो दशक बीत गया, कोई सम्मेलन नहीं हुआ। यह इस बात का उदाहरण है कि लघुपत्रिका आंदोलन में एक शिथिलता और जड़ता है। ऐसे में ‘प्रेरणा अंशु’ की पहल महत्वपूर्ण है, जिसने इस जड़ता और शिथिलता को तोड़ने का काम किया है।
आज नैतिक पतन के दौर में लघुपत्रिकाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज रचनाकार, वैचारिक लेखन से दूर होते जा रहे हैं जो समाज के लिए चिंता का विषय है। साम्प्रदायिकता का सवाल हो या धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न हो अथवा ग्लोबलाईजेशन का प्रश्न हो हमारी व्यावसायिक पत्रिकाएं सत्ता विमर्श को ही परोसती रही हैं। सत्ता विमर्श व उसके पिछलग्गूपन से इतर लघु पत्रिकाएं अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता, संघर्षशीलता व सकारात्मक सृजनशीलता की पक्षधर हैं। इन बातों के मद्देनज़र इतना स्पष्ट है कि लघु पत्रिकाओं की आवश्यकता हमारे यहां आज भी है, कल भी थी, भविष्य में भी होगी।