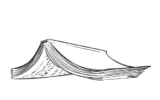भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भारतीय नागरिकों को न केवल स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की प्रमुख घटनाओं तथा अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्यपूर्ण संघर्षों व उनकी कुर्बानियों का सम्मानपूर्वक स्मरण करना चाहिए, बल्कि उस वैचारिक संघर्ष और अवधारणात्मक विकास को भी समझना चाहिए जो स्वतंत्रता आन्दोलन की विशेषता रहे हैं और उसकी उस क्रांतिकारी विरासत का निर्माण करते हैं जो आजादी के सात दशकों के बाद आज भी प्रतिध्वनित हो रही है। आज सत्तारूढ़ शासक हमारे गणतंत्र के संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे को रौंद रहे हैं और पूर्व के औपनिवेशिक शासकों के उत्तराधिकारियों की तरह हुकूमत कर रहे हैं, जिन्हें ‘भूरे अंग्रेज’ बताते हुए भगत सिंह ने हमें चेतावनी दी थी। ऐसे समय में हमें अपने स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रांतिकारी विरासत को फिर से समझना चाहिए ताकि हम फासीवाद से आजादी की अपनी जारी लड़ाई को ठीक से लड़ पाएं।
औपनिवेशिक युग में आजादी का पहला मतलब था औपनिवेशिक अधीनस्थता से मुक्ति। वह हमारा राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम था, और राष्ट्रीय मुक्ति के इस सपने की बुनियाद थे भारत के लोग, जो इस राष्ट्र के मालिक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूना में औपचारिक रूप से ‘पूर्ण स्वराज’ का प्रस्ताव लेने के काफी पहले ही भारत के उपनिवेश-विरोधी योद्धाओं ने राष्ट्र की आजादी और जन-संप्रभुता को सूत्रबद्ध करना शुरू कर दिया था। 1857 के राष्ट्रगान में भारत के लोगों को देश का मालिक घोषित किया गया था – ‘हम हैं इसके मालिक, हिंदोस्तां हमारा’। बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ ने युद्धघोष जारी किया ‘आबुआ दिशुम, आबुआ राज’ (हमारा राज्य, हमारा राज)। जन संप्रभुता अथवा जनता के हाथों सत्ता की भावना को संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक स्वीकृति मिली, जिसमें “हम, भारत के लोग” के साथ यह भावना भारत को संप्रभु गणतंत्र के रूप में ढालने का दृढ़संकल्प बनी रही। इस प्रकार, भारत और भारतीय राष्ट्रवाद के विचार के केंद्र में जनता ही है।
भारत की जनता हमेशा से विविधतापूर्ण रही है। यह विविधता – नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक – भारत की एकता का बुनियादी उसूल रही है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान परिष्कृत होते संचार माध्यमों और लगातार बढ़ती आवाजाही ने निश्चय ही जन-जुड़ाव को गहरा बनाया और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन इस एकीकरण को एकरूपता या समांगता की इच्छा समझने की भूल हर्गिज नहीं करनी चाहिए। एकरूपता या समांगता हासिल करने के प्रयासों ने हमेशा ही एकता को कमजोर बनाया है और इससे दुष्प्रभावित अंचलों और समुदायों ने इन प्रयासों को करारा जवाब दिया है। देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन ने कुछ हद तक इस विविधता को जरूर कमजोर बनाया, लेकिन यहां तक कि विभाजन के बाद का भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा विविधतापूर्ण देश है। स्वतंत्रता आन्दोलन ने भारत की विविधता के बारे में स्वस्थ समझ तथा आपसी सम्मान और स्वीकृति को विकसित किया। यही वह एकमात्र तत्व था जिसने भारतीय राष्ट्रीय एकता को बारंबार जीवन प्रदान किया और भारतीय राष्ट्र-राज्य के तहत (हिंदू व मुस्लिक शासकों की हुकूमत वाले) सैकड़ों देशी रियासतों के शीघ्र एकीकरण को सहज बनाया।
आजादी के अलावा, हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दूसरा प्रमुख शब्द था – इंकलाब यानि क्रांति, जिसे ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे ने अमर बना दिया। उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा गढ़े गए और भगत सिंह तथा उनके साथियों द्वारा अमर बना दिए गए इस नारे ने हमारा ध्यान आजादी के क्रांतिकारी महत्व तथा लगातार संघर्षों और प्रगतिशील बदलावों व अधिकारों के प्रति हमारी सतत जागरूकता की केंद्रीय अहमियत की ओर खींचा।
यकीनन, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो दूसरा नारा उछाला, वह था ‘साम्राज्यवाद मुर्दाबाद’। भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन अलग-थलग रूप से सिर्फ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं था, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी प्रतिरोध के अभिन्न अंग के बतौर विकसित हुआ था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद, जब यूरोप में फासीवादी प्रतिक्रिया को बढ़ते देखा गया, तो भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रगतिशील धारा ने यूरोप में फासीवाद-विरोधी प्रतिरोध का समर्थन किया। छह भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद, पत्रकार गोपाल मुकुंद हुद्दर, डॉक्टर अटल मोहनलाल, अयूब अहमद खान नक्शबंदी व मैनुएल पिंटो, और छात्र रामास्वामी वीरप्पन – जेनरल फ्रांको की अगुवाई में चलने वाली फासिस्ट सेना के खिलाफ लड़ने के लिए बने ‘इंटरनेशनल ब्रिगेड’ में शामिल हुए थे। लंदन में बसे भरतीयों ने फंड इकट्ठा किया और जवाहरलाल नेहरू ने एकजुटता जाहिर करने के लिए 1938 में स्पेन की यात्रा की। जहां आरएसएस मुसोलिनी और हिटलर से प्रेरणा ग्रहण कर रहा था, वहीं भारत के प्रगतिशील स्वतंत्रता संग्रामी यूरोप में फासिस्ट-विरोधी शक्तियों के साथ हाथ मिला रहे थे।स्वतंत्रता आन्दोलन का मकसद सिर्फ भारत में अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना ही नहीं था, बल्कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रगतिशील भारत का निर्माण करना इसका मकसद था।
आदिवासी और किसान समुदाय इस स्वतंत्रता आन्दोलन के सबसे बड़े जनाधार थे, और वे जमींदारों तथा सूदखोर महाजनों से मुक्ति के लिए लगातार लड़ रहे थे। आदिवासी विद्रोह और 1857 के स्वाधीनता युद्ध के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत ने सिर्फ सैन्य नियंत्रण और दमनकारी कानूनों के जरिये ही खुद को सुदृढ़ नहीं बनाया, बल्कि ‘स्थायी बंदोबस्त’ व अन्य राजस्व प्रणालियों के जरिये निर्मित जमींदार वर्ग द्वारा लागू सामंती सत्ता को मजबूत बनाकर, देशी रियासतों की सत्ता को बरकरार रखकर और हिंदू व मुस्लिम समुदायों के बीच ‘फूट डालो, राज करो’ नीति को जोरदार तरीके से लागू कर भी खुद को मजबूत बनाया।
उस जमाने के एक वरिष्ठ ब्रिटिश सैनिक अफसर ने स्पिष्ट कहा, “हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम पूरी ताकत से हमारे लिए फायदेमंद विलगाव को और बढ़ायें, जो विभिन्न धर्मों और नस्लों के बीच मौजूद है। ।।।फूट डालो, राज करो भारत सरकार का उसूल होना चाहिए” (लेफ्टनेंट कर्नल कोकर, ‘इंडिया टुडे’, रजनी पाम दत्त, 1940)। चंद सम्माननीय अपवादों को छोड़कर, ये जमींदार और देशी रियासतों के कठपुतली शासक औपनिवेशिक हुकूमत के सामाजिक आधार थे, और इसीलिए उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष को जमींदारों व महाजनों के खिलाफ किसान संघर्षों से बल मिलता रहा।
जमींदारी और सूदखोरी प्रथा का उन्मूलन औपनिवेशिक भारत में किसान आन्दोलन के प्रमुख नारे के बतौर उभरा था। चूंकि गांधीवादी सत्याग्रह आन्दोलन ने पर्याप्त जोर नहीं दिया और किसान जुझारूपन के हर प्रतीक से दूर हटता गया, इसीलिए किसान आन्दोलन ने अपना खुद का जुझारू मंच निर्मित किया। वह था अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में। यह किसान सभा 1936 में गठित की गई और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने। इसने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणापत्र जारी किया जिसमें जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने और ग्रामीण कर्जों को माफ़ करने की मांग उठाई गई थी। शक्तिशाली किसान संघर्षों ने न केवल ग्रामीण भारत में सामंती-औपनिवेशिक सत्ता को कमजोर किया, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंसा के खिलाफ भी वह एक प्रतिकारी ताकत बन गया। स्वतंत्रता के बाद, जमींदारी के पुराने स्वरूप को कानूनन खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके परे भूमि सुधार का काम अधूरा ही रह गया और अभी तो हम भूमि सुधार को उलटते हुए भी देख पा रहे हैं। औपनिवेशिक की जगह कॉरपोरेट रख दीजिये, और फिर हमलोग किसान आन्दोलन को कॉरपोरेट भूस्वामित्व और कर्ज संकट से जूझते हुए पाएंगे।
काम और जीवन की बेहतर स्थितियों के लिए संगठित होने व लड़ने के अधिकार समेत मजदूर वर्ग अधिकारों की लड़ाई भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रांतिकारी विरासत का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग रहा था। इन संघर्षों की बदौलत औपनिवेशिक काल में ही श्रमिक अधिकारों से संबंधित अनेक कानून पारित किए गए थे। फैक्ट्री कानून और ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926 से लेकर मजदूरी भुगतान कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून तक, भारत के कई प्रमुख श्रम कानून स्वतंत्रता के पहले ही बनाये जा चुके थे। 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ऐटक) और 1920-दशक से चले संगठित कम्युनिस्ट आन्दोलन के अलावा 1936 में डॉ। अंबेडकर द्वारा गठित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (आइएलपी) ने भी औपनिवेशिक भारत में मजदूर वर्ग के अधिकार हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आइएलपी ने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, दोनों को मजदूर वर्ग का दुश्मन चिन्हित किया था; और वह बंबई प्रेसिडेंसी में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के बतौर उभरी थी। उसने कई बड़ी चुनावी जीतें हासिल की थीं और विधान सभा के अंदर तथा व्यापक किसान-मजदूर संघर्षों में प्रमुख भूमिका अदा की थी।
1936 वह साल था जब दो क्रांतिकारी आह्वान जारी किए गए थे। जहां किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का आह्वान जारी किया, वहीं अंबेडकर जाति उन्मूलन के नारे के साथ सामने आए। जाति उन्मूलन के इस आह्वान ने सामाजिक न्याय के एजेंडा को सामाजिक रूपांतरण के उच्चतर स्तर तक असरदार ढंग से उठा दिया। छुआछूत मिटाने की सीमित गांधीवादी सारवस्तु से अलग हटते हुए अंबेडकर ने समूची वर्ण व्यवस्था को ही खत्म करने की जरूरत की तरफ भारत का ध्यान आकर्षित किया। श्रम विभाजन के नाम पर जाति को उचित बताने के प्रयासों को धक्का मारते हुए अंबेडकर ने जाति को श्रमिकों के विभाजन के बतौर देखा। जाहिर है, उसका जवाब जाति-विरोधी आधार पर श्रमिकों की एकजुटता ही हो सकती थी जिसके जरिये जातियां वर्ग के अंदर विलीन हो जाएंगी। इन क्रांतिकारी विचारों – जमींदारी उन्मूलन, जाति उन्मूलन और श्रमिकों की एकजुटता – का समागम वर्गीय एकता और वर्ग संघर्ष को काफी बड़े पैमाने पर ले जाने की क्षमता रखता था, लेकिन इस संभावना को उस वक्त साकार नहीं किया जा सका। ठीक यहीं पर हमें इस अधूरी रह गई संभावना और स्वतंत्रता आन्दोलन की इस विरासत को आज के भारत में पुनः तलाश करने की जरूरत है।