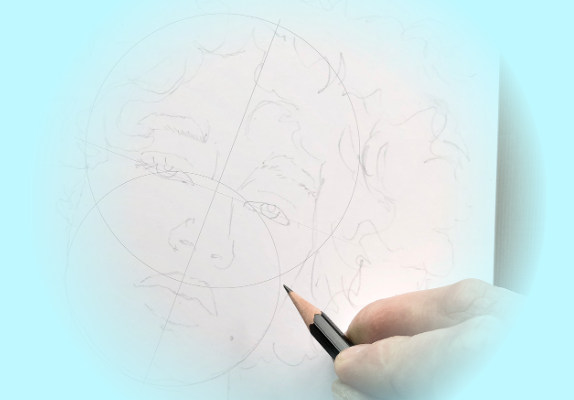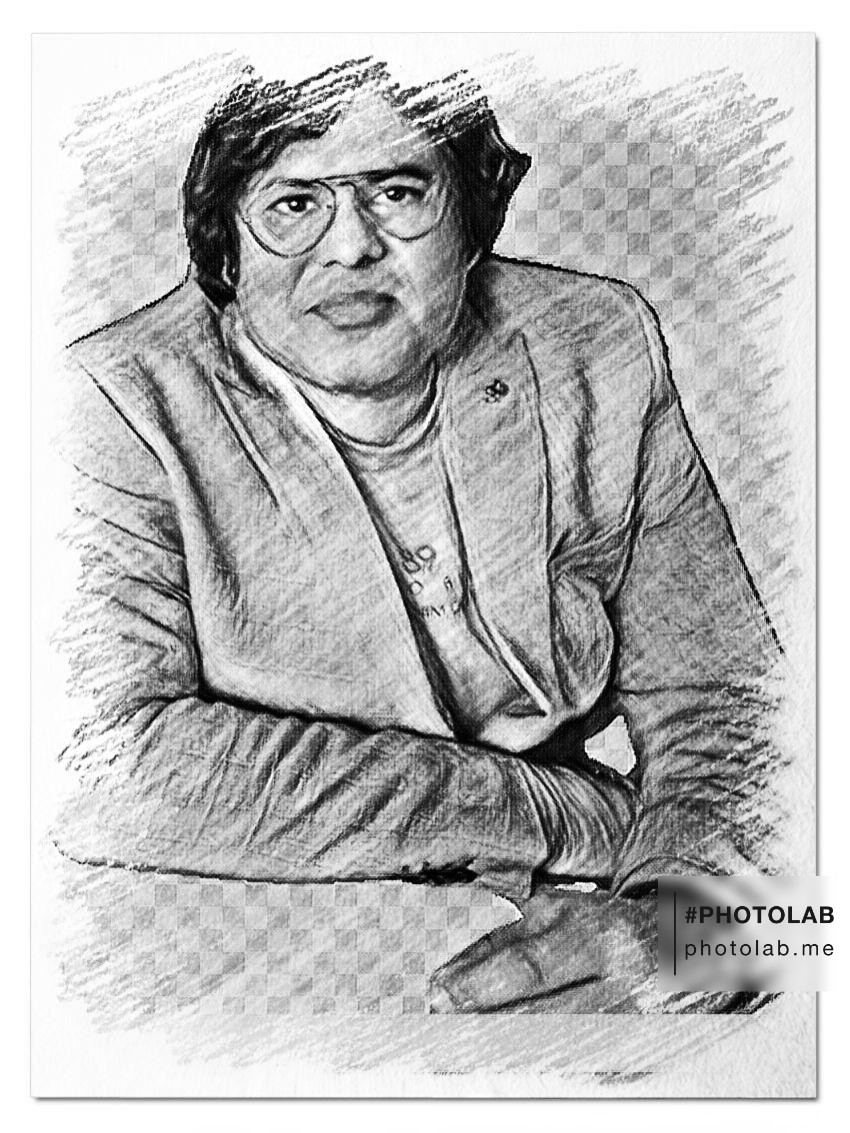नई सुबह, नई किरण
माँ-पिताजी की परेशानी ये थी-कितने प्रयास किये, कितना पैसा लगाया, सब व्यर्थ। मेरा मन अब इतना सहज हुआ कि इलाज अब और नहीं, जिसे दूसरी तरह से कहें तो-‘फेड़अप होना’ भी कहा जा सकता है।
पुरानी सड़कों पर जब रास्तें नहीं मिलते तो नई सड़कों की तलाश में भटकने का भी मन नहीं होता,यह सब आप अपने लिए सोच सकते हैं मगर तब-जब आप अपने लिए खुद फैसले लेने लगें। अभी वक़्त वैसा नहीं था।
किसी ने बताया कि बुढाना कस्बे में बस स्टैंड के पास एक देशी वैद है जो पोलियो का इलाज करता है। बस फिर क्या था- पिताजी और माँ उस वैद के पास ले चले। जब किसी का अंग-भंग होता है तो शायद उसकी सम्वेदना का स्तर भी बढ़ जाता है, शायद उस अंग विशेष की ताक़त भी मस्तिष्क में चली जाती हो। चुनांचे मेरा मस्तिष्क शीघ्रता से परिपक्व हुआ। वैद ने कहा था- लड़का तीन साल में सड़क पर दौड़ेगा, आप यहीं इसी बेंच पर बैठे हुए देखोगे।कल्पना ने एक चित्र खीचा- जैसे सड़क पर पहले धीमे क़दमों से, फिर थोडा सामान्य क़दमों से मैं सडक पर चल रहा हूँ, माँ-पिताजी देख रहे हैं, मुझे चलते हुए, उनके चेहरे पर संतोष के भाव हैं, मैं मन ही मन प्रसन्न हूँ।
वैद हर तीसरे दिन बुलाता, तेल की मालिश करता और फिर पट्टियों को लपेट देता। पट्टियों के नीचे लकड़ी की खरपच्चिया होती। खरपच्चियों से चुभन बहुत परेशान करती। मेरा मन बाहर दोस्तों के साथ खेलने का करता। मैं दीवार पकड़ कर चलने का प्रयास करने लगा।
वैद की सलाह पर पिताजी बढई से लकड़ी का एक गडुलना बनवाकर लाये। गडूलना बच्चे को सात-आठ महीने की उम्र में चलने के लिए दिया जाता है, हाँ, मैं भी उस पल इसी अवस्था में था, जब एक-एक कदम धीरे-धीरे उठाकर जमाकर चलने का प्रयास किया जाना था।मैं अब गडुलने की सहायता से चलने का प्रयास करता। हर पंद्रह दिन में वैदजी पैरों पर प्लास्टर चढ़ा देते, दो-तीन दिन चलना-फिरना बन्द हो जाता। अब मैं घर से बाहर कुछ कदम रखने लगा, अनुभव हुआ कि दुनिया इस चारदीवारी से भी आगे है। इसी समय माँ मेरी पहली शिक्षिका बनी, घर के काम-काज करते हुए पीढ़े पर मुझे बैठा लेती और पढने को कहती। प्लास्टर और पट्टियों के बीच जूझता बालक कैसे पढाई में मन लगाये, ये बात मैं माँ को नहीं बता पाता। माँ एक सख्त शिक्षिका थी, हिंदी के कायदे का काला पन्ना जो किसी के भी होश उड़ा दे, माँ चाहती कि मुझे वो काला पन्ना कंठस्थ हो। काले पन्ने के लिए मार भी लगती।
उम्र बढ़ने से शरीर का वजन बढ़ना भी वैज्ञानिक नियम है। माँ ने अधिकतर लम्बी से लम्बी दूरी को पैदल ही तय करना होता था। वह रिक्शा कभी नहीं लेती थी। बढती उम्र के बच्चे को माँ गोद में लेकर चलती,इसमें पट्टी और प्लास्टर का वजन भी जुड़ रहा था। माँ बड़ी मुश्किलों से ढाई-तीन किलोमीटर दूर बस अड्डे तक ले जाती और वहाँ से बस से बुढाना ले जाती। अब ये सब जिन्दगी का एक हिस्सा बन गया।
वैदजी जब भी प्लास्टर काटते- पंद्रह दिन पैर खुले छोड़ देते, बस दोनों पैरो के बीच दो जगह पट्टियों के बन्ध लगाये जाते ताकि पैर इधर-उधर न हों, प्लास्टर खोलने के बाद नीम के पत्तों के गर्म पानी से सिकाई होती ताकि जोड़ जाम न हो जाये, पैरों के जोड़ खोलने के लिए व्यायाम करना पड़ता।मैं एक ही काम रोज़-रोज़ करने से कई बार उकता जाता। तब माँ की सख्त हिदायत होती- ‘मेरे बेटे, ठीक होना है न, दूसरे बच्चों की तरह चलना है, फिर ये सब करते रहो।‘
दो घटनाएँ एक साथ घटी- माँ वैद के पास से वापस आ रही थी। माँ ने एक चाचा की साईकिल पर मुझे बैठा दिया। गॉंव के बाहर ही साईकिल रोक वे खेलने लगे साईकिल डगमगाई और धडाम से नीचे गिर गयी। बांए हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गयी। माँ आई, सुनकर बहुत गुस्सा हुई, उस दिन बहुत तमाशा हुआ। गॉंव में कोई थे जो हड्डियों के उतरने पर चढ़ा देते थे, उन्हें बुलाया गया, उन्होंने कहा-‘कोहनी उतरी है’, हिला-डुला कर कुछ किया और लुडपुड़ी बनवाकर बाँध दी। दर्द के मारे मैं कराहता रहा। अगले दिन सुबह होते ही पिताजी डाक्टर के यहाँ ले गए। अब हाथ पर भी प्लास्टर बंध गया था। मैं हाथ और पैर दोनों पर प्लास्टर देख रोता रहता।
दूसरी घटना ये हुई- अभी हाथ पर प्लास्टर बंधा था, माँ वैद से मेरा इलाज करवाकर आ रही थी, पैसे बचाने के चलते उसने उस दिन भी रिक्शा नहीं किया, वो मुझे गोद में ले वापिस आ रही थी। रास्ते में रेलवे के फाटक पड़ते थे, ट्रेन आने का समय था, फाटक बन्द। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग फाटक के नीचे से निकलकर आते-जाते, माँ ने समय बचाने के लिए फाटक के नीचे से निकलने का प्रयास किया। एक फाटक पार करके दूसरा फाटक पार किया, पैर एक पत्थर से टकराया। माँ का संतुलन बिगड़ा, उसने अपनी कोहनी नीचे टिका दी ताकि मेरे हाथ का प्लास्टर नीचे न लगे, माँ जैसे-तैसे सम्भली, दो कदम ही चली कि पैर के नीचे केले का छिलका आ जाने से संतुलन बिगड़ गया, माँ ने फिर से कोहनी नीचे टिका दी। कोहनी लहुलुहान हो गयी, मेरी आँखों में से अश्रुधारा बह निकली।
एक बच्चे की स्थिति ये होती है कि वह किसी से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इन सब बातों से सीखता जरुर है। मेरे मानसिक और सामाजिक विकास पर इन दो घटनाओं का काफी असर हुआ। माँ के हाथों की चोट मुझे मानसिक रूप से परेशान कर गयी।
वैद ने हाथ और पैर का प्लास्टर काट दिया और पैरों पर पट्टियाँ बांध दी। फिर एक दिन एक भाई की साईकिल पर बैठाने के कारण मेरा पैर साइकिल के पहिये में आ गया। पैर लहुलुहान, तब पैर में ४ टांके आये। यानी पल-पल पर जिन्दगी कुछ सिखा रही थी।
वैद के इलाज से काफी परिवर्तन दिखाई देने लगे। एक दिन वैद ने प्लास्टर काटा और कहा-“जाओ सड़क तक घूम आओ।” मैं अवाक वैद को देखता रहा। उनकी कर्कश आवाज गूंजी -“सुना नहीं, चलो सडक तक घूमकर आओ।“
मैं पास में पड़े स्टूल को पकड़कर खड़ा हुआ था, बमुश्किल पहला कदम आगे बढाया, अगला कदम आगे रखने की हिम्मत नहीं हुई, पसीने की बूँदें कानों के पीछे से चूने लगी। सारी हिम्मत बटोर अगला कदम बढाया, पैर मानो लड़खड़ाये। अगले पल बिजली के झटके से इलाज के दृश्य मस्तिष्क पर उभर आये। जिस दिन भी बिजली के झटके दिए जाते उस दिन मैं रोता-चिल्लाता और उस वैद को मन ही मन गालियाँ देता। आगे कदम बढ़ाना मज़बूरी थी। बमुश्किल चार-छः कदम अपने बूते रखे और फिर लड़खड़ा गया। पैर मुड़े तो दर्द से बिलबिला गया। १५ दिन प्लास्टर में सीधे रहने के चलते जोड़ लगभग जाम थे। मैं दर्द से बिलबिलाता रहा, माँ का हृदय चीत्कार उठा, वह उठाने को आगे बढ़ी, वैद ने रोक दिया-“नहीं बहन जी, आप नहीं उठायें, आज आप उठा देंगी फिर कहीं ऐसे गिरेगा, जहाँ कोई नहीं होगा, तब कौन उठाएगा?”
माँ आगे बढ़ते-बढ़ते रुक गयी। वैद की आवाज फिर कानों में पड़ी-“उठो और मेरे पास आओ।“
मैं जैसे-तैसे उठने का उपक्रम करता रहा, चीख और आँसू दोनों बदस्तूर जारी थे। लेकिन उठना मेरी जरुरत भी थी और मज़बूरी भी। १५ मिनट से भी अधिक समय तक मैं जूझता हुआ जैसे-तैसे उठा। लगभग लड़खड़ाते हुए मैंवैद के पास तक आया, पसीने से तरबतर।
जैसे ही वैद के करीब आया उसने कहा- “शाबास, लेकिन ध्यान रहे, अगली बार से गिरना नहीं है।” वैद ने दोनों पैर आपस में पट्टियों से बांधे और अगले हफ्ते आने को बोला।
माँ की आँखों में एक चमक को मैंने महसूस किया और खुद के मन में एक अजीब सा खौफ़, अगली विजिट का भय, फिर से वैद या तो बिजली लगाएगा या फिर से १५ दिन का प्लास्टर। यह इलाज दर्दनाक था, परिणाम क्या होगा ये बालमन को कैसे समझ आता, भय और खौफ़ के साए में समय बीतता, मैं हर अगली विजिट से पहले भयभीत होता।
अगली विजिट पर पट्टियाँ खोल वैद ने पैरो को मोड़ना शुरू किया, ज्यादा मोड़ने से दर्द हुआ, मैं चिल्लाया। वैद के डांटने पर सहमा हुआ बच्चा और सहम गया। पैरो के जोड़ का घर्षण कम करने के लिए वह उन्हें मोड़ता, मेरी चीख निकलती। उसने बिजली की मशीन उठाई, मैटल की करंटयुक्त छड़ियाँ देख रूह कांपने लगी,जैसे ही पैरो पर फिराना शुरू किया, मैं बिलबिला उठा। कितना सहन करता? वैद के ऊपर चिल्लाना शुरू किया-“ओ ढोंगी छोड़ मुझे, कुत्ते मुझे मारेगा? तू वैद नहीं कोई राक्षस है, तू ढोंगी है, मुझे नहीं इलाज कराना तुझसे। तू मुझे मारना चाहता है।”
मेरे मुँह पर चांटे पड़े। मैंने उसके हाथ पर दांत गडा दिए। माँ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वह भी मुझे दुश्मन लगी। वैद अपना काम करता रहा। ये दिन जिन्दगी का कितना दर्दनाक दिन था, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। माँ ने घर आने पर पूरा वाकया पिताजी को सुनाया, वे भी आश्चर्य में पड़ गए। माँ–पिताजी दोनों परेशान। इस समस्या का क्या हल हो, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया।
हमारे समाज की संरचना ऐसी है कि लोग किसी भी परेशानी में कितने ही एंगल खोज लेते हैं। पास-पड़ोस के कुछ खुसर-फुसर न हो ऐसा कैसे हो सकता है- बेटे के इलाज के नाम पर गुलछर्रे उड़ाती है, शर्म नहीं आती, बेशर्म औरत। यानि किसी मज़बूरी, नौकरी, पढाई के लिए बाहर निकली औरत बेशर्म है, चरित्र से ख़राब है। घर में भी माँ को कई बार आभास हुआ कि कुछ है जो पिताजी को खटक रहा है, कुछ है जिसकी वजह से वो घर में सहज नहीं हैं।
२१दिन का प्लास्टर था, इस बार पिताजी वैद के पास लेकर गए। उन्होंने मेरी गलती के लिए शर्मिंदगी जाहिर की और इलाज बन्द न करने की मिन्नतें की।
वैद ने कहा- “बच्चे की नादानी से मैं इलाज छोड़ दूँगा आप ये कभी मत सोचना। एक दिन इसे विश्वास होगा कि वैदजी उसके लिए राक्षस नहीं, शुभचिंतक हैं।“
पिताजी एक साथ दो घटनाओ से बेहद दुखी थे, मेरा वैद के साथ अभद्र व्यवहार और इधर पड़ोस की अफवाहें। उन्होंने मुझसे पूछा-“बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम्हें वैद से इलाज कराना है या नहीं?
मैंने इनकार में सिर हिला दिया। दुखी हृदय पिता ने बच्चे के पक्ष में अपना मत देकर इलाज बन्द कर दिया।
हम कितनी विवशताओं में जीते हैं, आज मैं इन घटनाओं के विश्लेषण, विवेचन में पड़ना नहीं चाहता, इतना काफी है कि आज जितना चल-फिर पाता हूँ उसमें अधिकांश योगदान उस वैद का है, जिससे जिन्दगी ने फिर मिलने का मौका न दिया, कुछ दिनों पहले मैंने धन्यवाद देने के लिए उस वैद की खोज की, वैद तो न मिले हाँ, उनकी मृत्यु का समाचार अवश्य मिला, समाचार सुन आँखों के पोर गीले भी हुए थे, शायद अंतिम श्रद्धांजलि के लिए मेरे पास आँसुओं के अलावा अन्य वस्तु उन्हें देने के लिए और थी भी नहीं।
मैं बहुत छोटा था, जब पोलियों के वायरस ने मेरे शरीर पर एक ग्रहण लगाया। जब मैं देहली पर बैठता- आते-जाते लोगो को तकता रहता, उन्हें चलते-फिरते काम करते देखता, लगता-इन राहों पर कहीं मेरा भी नाम लिखा होगा……।
उन रास्तो पर मेरे चलने के अरमान बिखर जाते, और तब लगता कि दो ही बातें हैं या तो अरमानों की जय हो या फिर बाधाओं पर विजय, इस जय और विजय में दो अक्षरों का मिश्रण था, “ज” और “य” इनमें एक अक्षर मैंने खुद से मिलाया “त” और तब कहीं एक नया शब्द बना “ज्योति”। वक़्त की चाल के साथ उम्र का बढ़ना लाजिमी है, इसी उम्र ने दस्तक दी तो माँ को लगा- नौ वर्ष की उम्र तक स्कूल नहीं, पास के स्कूल में नाम लिखाया तो यह तीन अक्षर ज,य.त का साथ हुआ और ‘ज्ञान की ज्योति’ मन और मस्तिष्क पर पड़ने लगी।
कैरियर की जद्दोजहद में जब एक स्थायी नौकरी को छोड़ दिल्ली चला आया, खालसा कॉलेज में किसी एग्जाम की ड्यूटी थी, यह एक शब्द जो तीन अक्षरों का मैंने यूँ ही चुन लिया था उसी नाम की सुन्दर बाला, साढ़े पाँच फीट से ज्यादा हाइट की वह लड़की- साथ में ड्यूटी करने आई पूछने पर उसने नाम बताया-‘परमज्योति’। यह एक शब्द मेरे लिए वरदान जैसा था। यानि ‘चोली-दामन’ जैसा साथ, इसी ‘ज्योति’ के दम पर मैं सूरज, चाँद, तारों तक में अपना अक्श, अपना भविष्य तलाशने लगता, कलम जो पकड़ी- चलते हुए हर पल को दस्तावेजी बनाने लगी। जीवन-संघर्षो से गुजरते हुए, ठोकरे खा आगे बढ़ते हुए एक मुकाम आया, साहित्य लिख रहा था, वही एक शब्द साथ था -ज्योति, जो ज्ञान-ज्योति के रूप में साहित्य में लगभग स्थापित करने में मेरा साथी रहा। जीवन ज्योति न सही, एक हमसफर न सही, लेकिन ये शब्द भिन्न-भिन्न रूपों में मेरे साथ मेरे संघर्षों के साथ चलता रहा। इस साहित्यिक सफ़र में एक बात ये हुई कि ये रिश्ता ऐसा हुआ, मेरा और परमज्योति का रिश्ता, जिसे शायद ही कोई समझ पाए। इसे मैं नेहरु-एडविना, अमृता-साहिर, राजेन्द्र-मीतु, जैसे नामों की तरह देखने की तामीर भी नहीं करता, समाज में कितनी प्रेम-कहानियाँ हैं जो न किसी मंजिल तक पहुँची, न ही उन्हें कोई नाम ही दिया जा सका। नेहरु-एडविना के रिश्ते में तन नहीं था, मन प्रमुख था, राजेन्द्र-मीतु के रिश्ते में तन प्रमुख रहा या सिर्फ मन ये राजेन्द्र के साथ ही चला गया, अमृता-साहिर का प्रेम तो जग जाहिर है, अमृता ने अपनी आत्मकथा में लिखा है-“मेरे और साहिर के रिश्ते के लम्बे बरसो में कभी तन नहीं रहा था-सिर्फ मन था- जो नज्मों में धडकता था।
मेरा और परम का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जहाँ मन अधिक था, लेकिन तन की भी वहाँ मनाही नहीं थी, जितना जब उसने खुद को खोला, और मुझे कॉल किया उतना ही मैं खुलता गया। ये रिश्ता मेरी शुरुआती कहानियों में कागजों पर अंकित होता रहा। अलग-अलग कहानियों की शक्ल अख्तियार करता रहा। हाँ, मैं अगर साहिर नहीं था तो इमरोज होना मेरे बूते नहीं था, नहीं जानता साहिर होने के मायने क्या हैं लेकिन इतना अवश्य ज्ञात है कि इमरोज दूसरा हो ही नहीं सकता।
वह जब भी मुझसे मिलती हम साथ होते, साथ घूमते, खाते-पीते और जब समय जाने का होता, मैं ऑटो रिक्शा से उसे छोड़ने जाता, उसे छोड़कर आते हुए मन बहुत उदास, बहुत मायूस होता। ऐसा कई बार होता, जब मिलकर बिछुड़ना होता, परम की बातें मन को बेचैन करती, मन का प्रेम मन को आहत भी करता, लेकिन उन पलों को उससे शेयर न कर उन पर कहानियाँ खूब लिखी। कविताएँ भी लिखी, नज्में तब तक नहीं लिखी थी। एक बार कहा- एक पूरा कविता संग्रह तुम्हारे नाम से निकालता हूँ। कविताएँ टाइप होकर प्रूफ भी पढ़े जा चुके थे लेकिन फिर क्या हुआ, प्रकाशक ही लापता हो गया। फिर बाद में उसी के नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किया, उस प्रेम पर एक कहानी लिखी, लगता था कि हम दोनों एक-दूसरे की परछाई हैं, कहानी थी- “परछाई पीछा नहीं छोडती”।
स्वयं से प्रेम करना सबसे बड़ी क्रांति है, ऐसा कहीं पढ़ा था, स्वयं को जानने की शुरुआत से अब तक के सफ़र ने इस बात को पुख्ता भी किया। हाँ, उस क्रांति की आग को अपने अन्दर सुलगाने की कुव्वत कितने इंसानों में होती है, ये अधिक महत्वपूर्ण बात है।
हमारा अतीत हमें वर्तमान में जीने के लिए तैयार करता है। अगर आप मुझसे अभी प्यार करना चाहते हैं, तो आपको मेरे अतीत को समझना होगा। क्योंकि जिन मुसीबतों से हो कर मैं गुज़रा हूँ, उन्ही की वजह से आज मैं सब कुछ हूँ।
पहली बार प्रेम जिससे हुआ वह तब नौवीं या दसवी क्लास में पढ़ती थी, वह मुझे चिट्ठी लिखती, जिनमें एक दर्द था, वेदना थी, परिवार में उपेक्षा का दंश दीखता था। चिट्ठियों का आदान-प्रदान एकदम नि:स्वार्थ था, जिसमें भावना थी, स्नेह था, वह आने वाले जीवन की कौन सी कड़ी बनेगा और बनेगा भी या नहीं, ये सोचा न था। मेरा चिट्ठी लिखना जवाबी होते हुए भी जज्बाती होता गया। मुझे लगता कि उसे एक वैचारिक साथी की जरुरत है, ख़त के माध्यम से विचारो का ये आदान-प्रदान का क्रम जारी भी रहा। हाँ, उसने ही मेरे मन में पहले-पहल प्रेम के अंकुर रोपे।
उसका प्रेम क्रान्तिकारी प्रेम था, मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण कि किसी लड़की के साथ पहली बार इतना नजदीक, इतना आत्मीय रिश्ता कायम हुआ। कालांतर में लगा कि शायद दोनों का ही तरीका गलत था। उसकी जिन्दगी में भी हिचकोले बहुत हैं और अपना भी कमोबेश यही मुकद्दर है।
वक़्त ने ये भी सिखाया कि इन्फ़ेचुएशन और प्लेटोनिक लव में क्या अंतर है? उम्र के नाजुक मोड़ पर सभी को एक भावनात्मक साथ की तलाश होती है, और वहीँ से कई बार रूहानी रिश्ते भी पनपते हैं, पता नहीं होता कि कौन, कब जिन्दगी में प्रवेश करेगा और कितना और कहाँ तक साथ चलेगा। यही वजह है कि लोग वक्त के साथ छूट जाते हैं लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनके साथ बिताये पल बहुत याद आते हैं।
मंजू मेहरा का जीवन में आना ऐसा था जो बहुत कुछ सिखा गया, उसने एक सबक ये सिखाया कि विवाह के लिए अपाहिज होना सबसे बड़ा गुनाह है, उसने बड़ी आसानी से कह दिया था- कौन बेवकूफ मां- बाप होंगे जो एक अपाहिज लड़के को अपना दामाद बनायें! ये बड़ा सबक था फिर परम ने भी अंतिम मुलाकात के वाक्य यही कहा था कि मेरे पेरेंट्स एक डिसेबल को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, थ्री गर्लफ्रेंड्स उपन्यास में ये तीनों नायिकाओं के रूप में उपस्थित हैं।
साहित्य में पदार्पण जिसकी मार्फ़त हुआ, वह अब साहित्य की दुनिया में न के बराबर थी, उसके विवाहोपरांत मिलना-जुलना तो छूट ही गया था लेकिन छोटी-बड़ी पत्र-पत्रिकाओं में उसकी अनुपस्थिति भी खलने लगी थी। इधर लगातार लिखना जारी रहा, ‘महक अभी बाकी है’ का सम्पादन किया तो मन में एक हूक उठी- आज सम्पर्क होता तो वह भी इस संकलन का हिस्सा होती।
इस बीच जो उपन्यास और कहानियाँ लिखी गयी, उनकी पहली पाठिका होने का लाभ भी उसे मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो न सका। ये मलाल आज भी सालता है- वह हर कविता, हर कहानी पर जो टोकाटाकी करती, वह अब नहीं हो पा रहा था। पहला क्रिटिक मुझसे दूर है।
आवाज की दुनिया एक समय आकर्षित करती थी, लेकिन ऑडिशन के समय गले की दिक्कत के चलते वंचित रह जाना पड़ता। आवाज की दुनिया तो अपना न बना पाई अलबत्ता अक्षरों की दुनिया ने अपना लिया।
शुरू में काव्य-गोष्ठियाँ खूब की, ज्योति के साथ भी, उसके बिना भी। एक समय आया जब इन गोष्ठियों का आकर्षण नहीं रहा, एकांत में बैठ लिखने का जो आनन्द है वह आनन्द- इन गोष्ठियों में मुझे कभी नहीं आया। एक बात जरुर समझ आई, यहाँ लोग सुनने या कविता की समझ के चलते नहीं, बस अपनी कविता सुनाने के मकसद से आते हैं।
कागज पर लिखने या कीबोर्ड से टाइप करते साहित्य को उस समय कोई पढ़ नहीं रहा होता, देख नहीं रहा होता, वह हमारा नितांत निजी पल होता है, और सम्भवतः सबसे सुखद भी। मैं उस सुख के चरम को महसूस करता, आनंदित होता।
‘थ्री गर्लफ्रेंडस’ उपन्यास ने प्रसिद्धि दिलाई लेकिन उसकी एक नायिका, वह जो स्वयं थी, उसके पास इसकी सूचना तक न थी- एक समय साथ-साथ साहित्य रचने, जलसों में शिरकत करने, छपने, पत्रिका निकालने की मौन कसमें खाई, लेकिन अब जब एक मुकाम मिला तो इंसानों की भीड़ में मैं नितान्त अकेला था, उसके आने की दूर-दूर तक कोई आहट न थी।
नज्में, कविताएँ या कहानियाँ जो लिखी- उन्हें एक बार उसके सामने बोलकर पढना मन को संतोष देता- अब मुझे अहसास होने लगा- उसकी गैरहाजिरी में तकनीकी हाजिरी का विलय हो सकता है- यूट्यूब पर चैनल बना वहाँ साहित्य का वाचन करके अपलोड करना एक उपाय लगा, शायद इसी तरह कहीं कुछ उसके कानों तक पहुँचे। यही वजह थी- वाचन में लगातार कुछ अलग किया जाने लगा। शायद आवाज में उतरे अक्षर हमेशा के लिए ध्वनि-तरंगों के रूप में हमेशा के लिए वायुमंडल में जीवित रहते हैं। मन से एक आवाज आती- अक्षरों की दुनिया की नायाब दोस्त कभी तो मेरे ये अक्षर तुम्हारे आँचल को हिला हाले-दिल सुनायेंगे। वैसे तो जब से लिखना शुरू किया था, तब से ही मुखातिब भी हुआ लेकिन ग़ालिब अकादमी द्वारा सम्मानित और अभिनव मंच से “प्रेमचंद सम्मान” से अलंकृत हुआ तो टीवी और रेडियो के लोगों के साक्षात्कार के समय मैंने कहा- दोस्तों, ‘थ्री गर्लफ्रेंड्स’ ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचा दिया। और मन में उसका स्मरण किया, जिसने मुझे साहित्य की दुनिया से परिचित कराया।