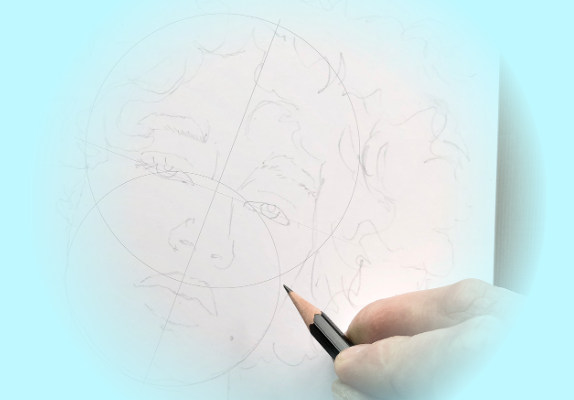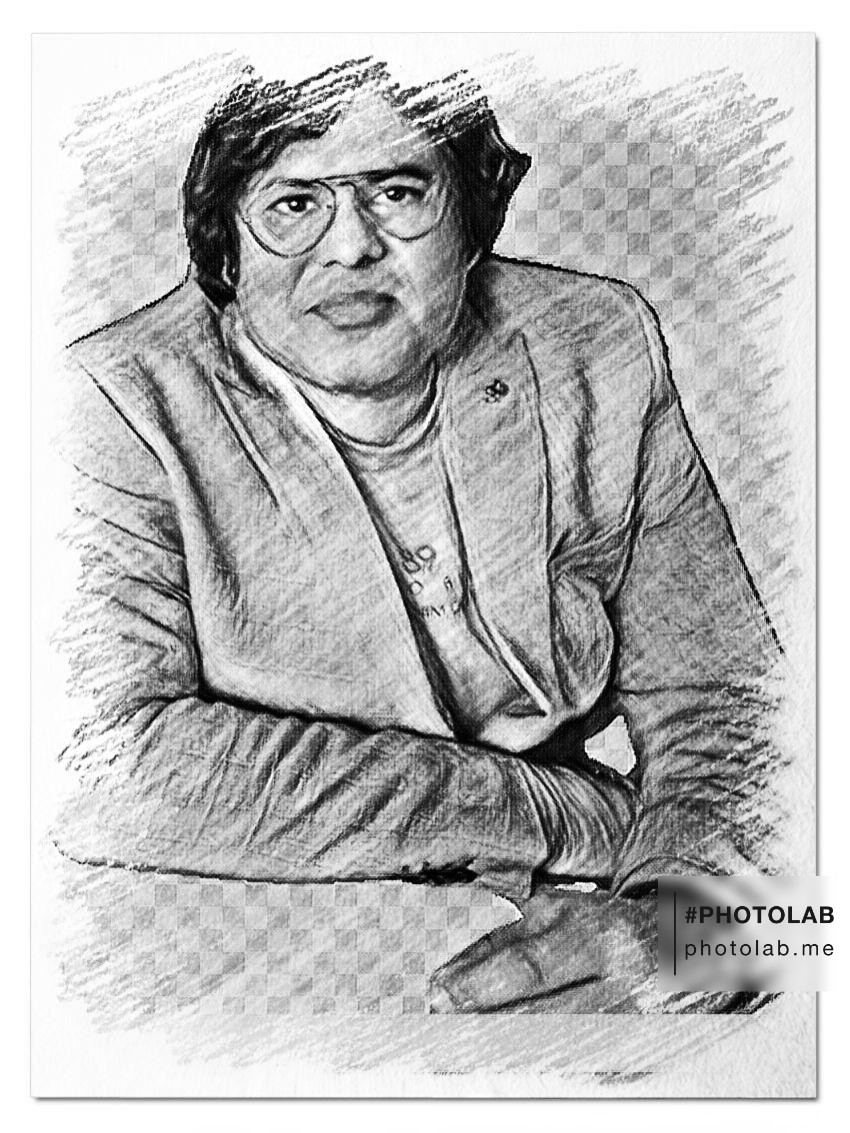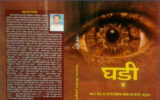मैं नहीं जानता कि कब मुझे पोलियो हुआ, बस माँ बताती है कि मैं ग्यारह महीने का था तब, खाट (चारपाई) पकड़ खूब तेज दौड़ने लगा था। शरीर से बहुत ही हष्ट-पुष्ट, फिर एक दिन मुझे तेज बुखार आया था, पिताजी और माँ मुझे साइकिल से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने थोड़ी जाँच के बाद कहा- “पोलियो हुआ है।” शिक्षक होने के नाते पिताजी जानते थे, पोलियो क्या बला है लेकिन माँ एकदम अनभिज्ञ थी।
खाट पकड़कर दौड़ने वाला लड़का अब खड़ा नहीं हो सकता था। ईलाज का सिलसिला शुरू हुआ, डॉक्टर, नीम हकीम, मौलवी, पंडित जहाँ जो कोई कुछ बताता माँ–पिताजी मुझे वहाँ लेकर जाते। मुझे बहुत सी घटनाओ की धुँधली यादें हैं, कुछ यादें घिनौनी भी हैं। यानि घोर अन्धविश्वास, लेकिन यकीन मानिये- जब किसी पिता को ये कहा जाए कि अब तुम्हारा बेटा कभी खड़ा नहीं हो पायेगा, चल नहीं पायेगा, तब वह पिता अन्दर तक कितना टूटता है, तब उसे अन्धविश्वास पर भी विश्वास करने को बाध्य होना पड़ता है। घोर अन्धकार में एक रोशनी की किरण को पाने की चाह ही उस सब पर विश्वास करने को बाध्य करती है, जिसके परिणाम सिफर ही होने हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही थी, पिता की चिंताएँ भी बढ़ रही थी।
मेरे शहर से कोई १८-२० किलोमीटर दूर एक क़स्बा है भोपा, वहाँ कहीं कोई बूढा था उसने एक बाग़ में अपना ठिकाना बनाया था, मैं बामुश्किल तीन साल का रहा हूँगा, मेरी स्मृति में उस बाग़ का पूरा दृश्य शेष है, बाग़ में एक ट्यूबवेल थी, साथ की प्लास्टिक केन की दुकानें थी, लोग केन को ट्यूबवेल के पानी से भरकर लाइन में लग जाते, बूढा सबके सिर पर हाथ रखता जाता, अब बोतल का पानी मरीजों को पिलाने को कहा जाता। वहाँ खूब चढ़ावा चढ़ता, और प्रचार ये कि बाबा कुछ माँगते नहीं, जिसकी जो श्रध्दा हो- वह दे सकता है। मुझे वहाँ कई बार ले जाया गया, बोतल में भर कर लाया गया पानी मुझे पिलाया जाता लेकिन इससे रत्ती भर भी फायदा नहीं होना था, नहीं हुआ।
औलाद का बीमार होना- दुनिया के बड़े ग़मों में से एक गम है। चेतन और अवचेतन में वो तमाम किस्से आज भी मौजूद हैं- कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे इलाज के तरीकों से गुजरना पड़ा। ऐसा ही एक किस्सा कुछ यूँ है-
गाँव के बाहर एक शिवालय है, जब से दो कुँए ढककर गॉंव के अन्दर मंदिर बने, लोगों का इस शिवालय में पूजा-अर्चना लगभग बन्द है- शिवालय एक बड़े बाग़ के बीचोचीच है। तो खबर आई कि एक पहुँचें हुए साधू आये हैं। साधू ने सरकारी ट्यूबवेल के पानी से बाग़ में पानी लगवाया तो बिलों के सांप बाहर आये, इसे भी एक चमत्कार में शामिल किया गया, शिवालय में शिव की मूर्ति पर सांप।
साधु घर आये और बोले- दस दिन, बस दस दिन और लड़का दौड़ेगा, सामान की लम्बी लिस्ट और लेप बनाकर पैरों पर बांध पट्टी कर दी। दो दिन बाद पट्टी खोल, दिखाया और कहा- देखो, घुटने के जोड़ मिलने लगे हैं। डूबते को तिनके का सहारा और उम्मीद, चमत्कार की आशा, ये सब मिलकर न हुए पर भी विश्वास को बाध्य करते हैं। लेप के लिए और जड़ी-बूटी लाने की पेशकस- धन की उगाही, ये उगाही अन्य कई परिवारों से भी हुई, दोपहर का भोजन कर साधु बाबा सामान लेने बाजार गए और शायद अंतर्ध्यान हो गए।
शिवालय अब भी पुनरुद्धार की बाट जोह रहा है। और मरीज अपने ठीक होने की आशा के साथ साधु का इन्तजार कर रहे हैं, हमारे देश में साधुओं पर विशेष श्रद्धा का चलन है, देश की सांस्कृतिक विरासत हमें इससे विमुख कब होने देती है।
इलाज और बस इलाज
जब पोलियो हुआ उस समय खतौली में बुखार और दांतों के डाक्टर के अलावा कोई अन्य इलाज भी नहीं था, कुछ वैद्य रहे हों तो याद नहीं, जब किसी की दवा से कोई आराम नहीं लगा तब पिताजी मुझे लेकर मुज़फ्फरनगर के नामी-गिरामी डॉक्टर सलूजा के पास गए। डॉक्टर सलूजा के क्लिनिक में पोलियो के मरीजों की भीड़ बहुत होती थी, ये भीड़ क्यूँ होती इसे शायद खुदा भी नहीं जानता, मेरा नम्बर आने पर डॉक्टर ने पोलियो को बेहद खतरनाक बीमारी बताया और इसका मेरे दोनों पैरों में भयंकर असर बता, इलाज लम्बा चलने की हिदायत दे डाली।
पोलियो के बारे में मैं जितना जान पाया वो ये कि यह एक संक्रामक रोग है जो पोलियो-विषाणु से मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। यह बीमारी बच्चों के किसी भी अंग को जिन्दगी भर के लिये कमजोर कर देती है। इसका वायरस मल पदार्थ से शरीर में जाता है। ज्यादातर वायरस युक्त भोजन के सेवन करने से यह रोग होता है। यह वायरस श्वास-तंत्र से भी शरीर में प्रवेश कर रोग फैलाता है। मैंने ये भी जाना कि पोलियो मॉंसपेशियों व हड्डी की बीमारी नहीं है बल्कि स्पायइनल कॉर्ड व मैडुला की बीमारी है। स्पाइनल कॉर्ड मनुष्य का वह हिस्सा है जो रीड की हड्डी में होता है। लोगो में ये भी भ्रान्ति है कि ये लकवा है, पोलियो वायरस ग्रसित बच्चों में से एक प्रतिशत से भी कम बच्चों में लकवा होता है। इसकी चपेट में बच्चों के आने का कारण ये है कि बच्चों में पोलियों विषाणु के विरूद्ध किसी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है इसी कारण इसका वायरस बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है।
जब डॉक्टर सलूजा के यहाँ इलाज शुरू हुआ- उसकी फीस १०० रूपये एक विजिट की हुआ करती थी और पिताजी की तनख्वाह बमुश्किल १५०-२०० रूपये माहवार। ये फीस पूरे महीने की न होकर एक बार मरीज को देखने की थी, अंदाजा लगाइए डेढ़ सौ या दो सौ रूपये महावार कमाने वाला व्यक्ति किन हालात में अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए बेबस हो सकता है?” माँ बताती है- लगातार दो साल तक डॉक्टर सलूजा का इलाज चलता रहा लेकिन कोई फायदा वहाँ से रत्तीभर भी नहीं हुआ।
किसी ने बताया कि दिल्ली के नारायणा विहार में एक डाक्टर हैं जो पोलियों का इलाज करते हैं। माँ-पिताजी दोनों मुझे लेकर नारायण विहार आ गए,वह बिजली के करंट से इलाज करता। उसे लगता कि बिजली की मशीनों से शरीर में झटके देकर खून का दौर पुनः चालू किया जा सकता है, इससे नसों में जमा खून फिर से शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है ऐसा डॉक्टर का कहना था। पिताजी को ये तरीका अजीब जरूर लगा लेकिन कहते हैं औलाद का दुःख ही माँ-बाप के लिए सबसे बड़ा दुःख होता है। एक आस की किरण की तलाश में वे जगह-जगह की खाक छान रहे। बस बेटे को कहीं से आराम लग जाए, ये ही उम्मीद लेकर उन्होंने इलाज कराने का फैसला कर लिया। घर का काम-काज करके माँ नारायणा लेकर आती, भाई-बहन स्कूल जाने लगे थे। इलाज में लगभग पूरा दिन खर्च हो जाता। माँ दिन भर का खाना बनाकर और पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करके ही घर से निकलती। गनीमत ये कि एक दिन छोडकर इलाज के लिए आना पड़ता, वरना दिक्कतें कहीं अधिक होने वाली थी। माँ अधिक दूरी भी पैदल ही करना पसन्द करती जिससे कि किराये में कम से कम खर्च हो। रिक्शा वह कभी नहीं लेती, सालों इलाज के बाद भी कोई फायदा नहीं था, मरीज आज भी वहीँ था जहाँ, बीमारी होने के पहले दिन था।
अब इलाज एक बार फिर बन्द था, हुआ ये कि एक दिन तेज बुखार आया- डॉक्टर भार्गव ने बुखार की दवा दी, फिर कहा- पैरो में पोलियों है? पिताजी के पुष्टि करने पर उसने कहा- मैं इलाज शुरू करता हूँ, तब लकड़ी की फट्टी के फ्रेम लेकर डॉक्टर टेप से पैरों को सीधा करके बाँधकर बीच में पट्टी बाँध दी, अब हर पन्द्रह दिन का ये सिलसिला बन गया। लकड़ी की फट्टी टेप से पैरो में बाँधना, न ही हिल सकता था, न ही टट्टी-पेशाब ही सही से कर सकता था। तकरीबन एक साल ये सिलसिला चला- परिणाम सिफर। इलाज एक बार फिर बन्द। यानी ये इलाज टुकड़ों में चलता रहा।
माँ को चिन्ता ये थी- न ही कोई फायदा हो रहा, न ही पढाई के लिए दाखिला हो पाया। ५ साल का हो गया लेकिन पेट के बल ही सरकता। हाँ, बस इतना सुधार आया कि अब घुटनों के सहारे घिसटकर जमीन पर चल लेता। मोहल्ले के कुछ बच्चे मेरे दोस्त बन गए। जो हमउम्र थे, उनसे ही दोस्ती हुई। छोटे-मोटे खेल खेलते, मेरा दिमाग तीव्र गति से चलता, ये बात पिताजी को समझ आने लगी थी। उनका मन कहता कि बच्चा थोडा भी खड़ा होने लगे तो इसे स्कूल भेजा जाये। कोई भी इलाज कारगर नहीं हुआ।
खेल और बाल मन
खेल हर बच्चे को हमेशा आकर्षित करते हैं, उस समय किसान परिवारों में पैसे का सदैव ही अभाव रहता था, कहते हैं मंदा जमाना था, खेलने के लिए खिलौने किसान परिवार में कम ही दिखते, हालाकि गन्ने की कैश-क्रॉप होने के चलते इधर अपने गॉंव में किसान की हालत कुछ बेहतर रही, “मेला छड़ियान” से जो खिलौने ख़रीदे जाते उन्हें साल तक सम्भालना होता। बाँसुरी, कैमरा, गेंद, माउथ-आर्गन, और कई तरह के प्लास्टिक के खिलौने, लेकिन ये सब रोज के खेलने के काम न आते। तब नए खेल इजाद होते। साईकिल के टायर, टूटी चप्पल के पहिये से बनी गाड़ी, सायकिल की ट्यूब को काटकर छल्ले बना, उनसे बनी बॉल से पत्थर की बनी गोल आकार की वस्तु बना उन्हें बॉल से गिराने वाले खेल मेरे लिए असम्भव से थे।
चूँकि मैं अब पेट के बल न सरककर, बैठकर घुटनों के बल कुछ तेज चलने लगा- दोस्तों के घर भी जाता, ये जो चलने का भोंडा सा तरीका इजाद हुआ इसमें मुझे कभी लज्जा जैसा नहीं लगा, एक खेल इजाद हुआ- एक बड़ी रस्सी के दोनों सिरे बांधे, मैं सबसे आगे होता, रस्सी मेरे गले में होती थी, मेरे साथी पीछे होते, रेलगाड़ी के डिब्बो की तरह, मानो ये एक स्लेज है और मैं उसे खीचने वाला कुत्ता, दोस्त पीछे से कुछ बोलते होते, तब शायद ये भी ज्ञान नहीं था कि वे मजाक बना रहे हैं या सिर्फ एक खेल है। आइस-पाइस जैसे खेल भी अभी मेरे लिए मुश्किल भरे ही थे।
पोलियो का इलाज तो 7 या फिर 8 साल की उम्र में बन्द हो गया। और एक दिन मेरा नाम स्कूल में लिखा दिया गया। पहली कक्षा से कहीं ज्यादा उम्र- सीधे चौथी कक्षा में दाखिला मिल गया। माँ-पिताजी की एक बड़ी चिंता का समाधान-स्कूल में दाखिला। घर पास-पड़ोस जिसके पास समय होता, स्कूल छोड़ आता। इस प्रकार स्कूल जाना शुरू हुआ। पहली ही परीक्षा में अच्छा करने पर जल्दी ही 5 वीं क्लास में प्रोमोट हो गया।
घुटने पर हाथ रखकर चलने की तकनीक भी खुद ही इजाद हुई, थोडा चलना-फिरना शुरू हुआ। अब जमीन पर घसीटकर नहीं चलना था, या फिर घुटनों के बल चलकर कपडे नहीं फटने थे, बस घुटने पर हाथ रखना था और चलना था, अब भी कपडे फटते थे, लेकिन सिर्फ घुटने से। चलना शुरू हुआ तो सोचता- काश मैं भी बल्लू के पेड़ के नीचे तक जा पाता। काही-पत्ता खेलना मेरे लिए दिवास्वप्न जैसा हो गया। शुरू-शुरू में गुल्ली-डंडा भी नहीं खेल पाता, फिर उल्टे हाथ से खेलने का अभ्यास किया। कुछ ही दिनों में गुल्ली-डंडे का चैम्पियन हो गया। अब बच्चो के साथ मैच लगाता और जीत जाता, बच्चे मेरे साथ खेलने और मैच लगाने से डरने लगे, जब भी खेलता दो-चार गुल्ली खो देता इतनी जोर से डंडे मारता कि गुल्ली किसी के भी घर में जा गिरती और फिर वापिस नहीं मिलती। कंचे खेलने में भी माहिर हुआ। लम्बे हाथ बड़ी-बड़ी अँगुलियाँ, पिल-चोट हो या गिट-नाप बच्चे अब जीत न पाते। मेरी अनोखी तकनीक से वो हार जाते। गुल्ली और कंचो का ‘मेजर ध्यान चंद’ बन गया था मैं।
घर में डांट पड़ती कि क्यों स्कूल से आते ही खेलने निकल जाते हो, घर पर पढ़ते नहीं। माँ को तो कह देता- आपको पढने से मतलब या अंक लाने से, देखती नहीं हो, अव्वल आता हूँ अपनी क्लास में, माँ कहती- ‘हाँ बना रह अन्धो में काना सरदार।‘
खेल भी उस एक घटना से ध्यान बाँटने का काम करते- जो घटना दिमाग में कभी डिप्रेशन तो कभी चैलेंज लिए खड़ी होती।
पराये जैसे अपने
मुकेश (बड़े भाई) के पैर की हड्डी टूटी थी, उसे प्लास्टर बंधा था, उसके पैर में दर्द होता तो वह कहता कि सन्दीप मेरा पैर अपने कन्धे पर रख, प्लास्टर के वजन में कन्धा टूटने जैसा लगता, मुकेश रोकर चिल्लाकर बार-बार अपना पैर मेरे कन्धे पर रखवा लेता, बड़ा होने के चलते उसकी दादागिरी हमेशा चलती, जब प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लगभग उसी समय पिताजी ने चौबारा बनवाया था, लेंटर खुल चुका था लेकिन छतबंदी नहीं हुई थी, दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं हुआ था, उस दिन मुकेश ने कहा-चलो आज ऊपर सोयेंगे, तब उसके पैर की हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर को काफी समय हो चुका था लेकिन प्लास्टर अभी कटा नहीं था, वह सीढियों से बैठते हुए ऊपर तक गया, हम सब लोग खाना खाकर ऊपर गए, रात को ऊपर सोने की प्लान बन चुका था, रात में तेज बारिश हुई तो हम लोग अन्दर कमरे में चले गए लेकिन लेंटर की छत भी टपक रही थी, शायद ये १९८२ की बात है, तब सीमेंट का कोई घोटाला हुआ था, कम्पनी ने घटिया सीमेंट जो शायद जम गया था उसे दोबारा पीसकर बोरो में पैक करके मार्किट के हवाले कर दिया था, इस घटिया सीमेंट के चलते छत टपक रही थी, चादर से मुकेश के पैर को पिताजी ने ढक दिया था, लेकिन बारिश न रुकने से पानी का टपकना बढ़ता जा रहा था, जिससे पैर का प्लास्टर भीग गया।
पिताजी ने बहुत गुस्सा किया, एक छोटे से खटोले पर मुझे लगभग पटकते हुए पिताजी ने कहा- “#%#%#%#”। उस वक़्त पता नहीं चला कि ये कौन सी भाषा थी और ये कौन सा गुस्सा था? एक बच्चे के प्लास्टर के भीगने की चिंता दूसरे बच्चे के अस्तित्व, उसके बालमन को आहत करने का सबब कैसे बनी- आज तक समझ नहीं पाया। आज जब ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ तब महसूस हो रहा है मानो सब कुछ चलचित्र की तरह आँखों के समाने चल रहा था, तब मेरी उम्र मात्र ६ या ७ साल रही होगी….।
ये मात्र एक घटना है जब घर से ही मन आहत हुआ.. कितनी ही बार उस माँ के मुँह से भी ऐसे शब्द सुनता-जिसने मेरे इलाज में अपनी उम्र और जवानी का एक बड़ा हिस्सा फूँक दिया, एक तरफ उनका त्याग, समर्पण, और पानी की तरह अपने इलाज पर पैसा बहाते देखता दूसरी तरफ ##%#%# जैसे शब्द सुनता तो समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है?
शायद हमारा समाज विकलांगो को लेकर बहुत संवेदनशील कभी नहीं रहा… संवाद की भाषा को समाज इजाद ही नहीं कर पाया, पड़ोस हो या घर अक्सर हर एक विकलांग को सभी से कटाक्ष भरे शब्द सुनने को मिलते हैं… लेकिन मन अधिक आहत तब होता है जब घर के लोग, अपने रक्त-सम्बन्धी ऐसे शब्द बोलते हैं… अपने ही भाइयों, बहनों, माँ-बाप से अपाहिज होने की गाली सुनने से ज्यादा आहत करने से अधिक घातक क्या होगा… मुझे याद है जब कभी मेरे बाबा खतौली से हमारे घर आते और कोई मुझे परेशान करता तो वो कहते, ये तो बिचारा पहले ही अपाज (अपाहिज ) है, क्यों इसको परेशान करते हो, यह शब्द मेरे अन्दर छूरी से अधिक गहरा घाव करता…। कोई अगर मुझसे परिचित नहीं है या पिताजी का कोई जानकार आता और मुझे, मेरी अवस्था को, मेरे घसीटकर चलने के पोस्चर को देखता और पूछता कि इसे क्या हुआ? तो अधिकांश जवाब में “बेचारा” और “अपाज” शब्दों का मिश्रण होना आम बात होती।
इन सबमें सबसे कष्टकर होता- सलाहवीरों का आकर कहना- टेलरिंग सिखा दो, किसी टीवी रेपियेर की दुकान पर छोड़ दो, परचून की दुकान खुलवा दो, गुजारा ही तो करना है, किसी गिरी-पड़ी लड़की से शादी हो जाएगी तो दो रोटी वक़्त पर मिलती रहेगी। यक़ीनन ये सलाहवीर हर काल, हर युग, हर समाज में होते हैं- बिना शुल्क सलाह देते हैं, और दिखावा सम्पूर्ण सम्वेदना का। समझना चाहता था- जीवन का उदेश्य क्या है?- दो रोटी पाना, शादी करके बच्चे पैदा कर लेना? या फिर अपने हिस्से का जीवन भरपूर होकर जीना?, क्या है जीवन?
अष्टावक्र के बारे में कहीं पढ़ा था- इनका नामकरण ही इस आधार पर ‘अष्टावक्र’ हुआ -‘आठ जगह से टेढा’, ऐसे टेढ़े-मेढ़े शरीर प्राप्त करने के बावजूद इन्होंने हार न मानी और परम प्रतिभा का परिचय देते हुए जग समादृत विद्वान बने। कहते हैं उन्होंने अपनी विकलांगता पर तनिक भी मन छोटा नहीं किया था। उन्होंने ऐसी विद्वता हासिल की थी कि इस पर सोचना और दुखी होना उनके लिए शोभा नहीं देताथा। उनके बारे में जो कथा पढ़ी वह यह थी- राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ को गए अष्टावक्र पर सभासद उनके चलने की दशा को लेकर हँसने लगे, जब सभासद अष्टावक्र को देखकर हँस रहे थे तो अष्टावक्र सभासदों पर हँसें, ऐसी विचित्र स्थिति में राजा जनक ने अष्टावक्र को पूछा -‘हे बालक! सभासद की हँसी तो समझ आती है, लेकिन तुम क्यों हँस रहे हो? मात्र बारह वर्ष के बालक अष्टावक्र का जवाब सुनकर सभी दंग रह गए। अष्टावक्र ने कहा– ‘मेरे हाड़-मांस की वक्रता पर हँसने वालों की वक्र-बुद्धि पर मैं हँस रहा हूँ। ये सभी लोग मानसिक वक्रता से पीड़ित हैं, ये विद्वान् तो कतई नहीं हो सकते, इसीलिए मुझे हँसी आ रही है!
ऐसे वक्र बुद्धि जीवन पर्यंत मिलते हैं, अक्सर मुझे भी मिलते रहे। मेरे ट्रेनिंग प्राचार्य से लेकर दिल्ली विश्विद्यालय के कुछ एक सीनियर, एडहोक फैकल्टी के मनोज झा और यहाँ तक कि ‘कथा संसार’ पत्रिका के संपादक ‘सुरंजन’ जैसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, जिनसे शारीरिक वक्रता के चलते बेइज्जत होना पड़ा।
सुरंजन को एक अंक पर मैंने टीप लिखकर भेजी, एनबीटी की पुस्तकों पर उसके ‘कचरा विचार पर’ उसने जवाब में मुझे पत्र लिखा-
भाई सन्दीप,
तुम्हारी प्रतिक्रिया पढ़ी, चाहता तो चुप रहता रहता पर दिल नहीं माना यह लिखने को कि तुम्हारी बुद्धि पर मुझे दया आती है, और तुम्हारे व्यक्तित्व पर हँसी! ऊपर वाला सचमुच तुम्हारा मजाक उड़ाया है। काश, उसने तुम्हें समूचा बनाया होता पर उसने आधा-अधुरा बना दिया।… पहले अपने भीतर झाँको, तुम कितने निर्मल हो…! …मेरे जैसा जीवन तुम सात जन्म भी नहीं जी सकते। सब तुम्हारी सोच जैसा सोचे यह सम्भव नहीं है। …तुम्हारा पत्र जरुर छापूँगा। इत्मिनान रखो। शेष फिर…
सुरंजन
२० जनवरी ०५
व्याकरण की भरपूर त्रुटि वाला ये पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित है। इसका जो शेष फिर था वह “कथा संसार” के एक अंक में कुछ यूँ आया कि किसी ऐसे क्षद्म नाम से सुरंजन ने एक पत्र खुद लिखकर छापा, जिसमें मेरी शारीरिक-वक्रता पर भद्दे-भद्दे मजाक किये गए थे।
सुरंजन एक ऐसा गुमनाम व्यक्ति था, जिसे साहित्य में लोग न के बराबर जानते थे, मैंने अपनी पुस्तक के विमोचन में उसे मुख्य अतिथि बुलाया तो उसने लडखडाती जुबान में कहा था-“मुझ अपरिचित नाम को मुख्य अतिथि बुलाकर, मेरा सम्मान किया, मैं ये सम्मान नहीं भूल सकता।“ उस अपरिचित पत्रिका के प्रोमोशन और आर्थिक सहयोग पर सुरंजन बेहद खुश भी हुआ लेकिन फिर ये सब देख उसके और उस जैसे लोगो के विचारों ने विचलित अवश्य किया।
तीन प्रेमिकाओं में से दो का इसी वक्रता के चलते शादी से इन्कार भी एक समय जरूर मन:वेदना का कारण बने, कालांतर में इन सबके बाहर निकलने की असीमित उर्जा का संचरण हुआ, ये उर्जा अकारण न उपजी, इसके मूल में लोगो की हेय दृष्टि ही रही। ऐसे नकारात्मक लोगों के चलते ही ‘मैं किसी से कम नहीं’ वाली धारणा ने मन के अन्दर एक दबंग इन्सान को जन्म दिया।
कैसे कैसे कष्ट
उन दिनों गाँव में किसी के यहाँ फ्लश नहीं होते थे… एक दुबारी थी, जिसके किवाड़ नहीं थे, उसमें चोखट थोड़ी ऊँची थी, मुझे हाजत लगने पर उस चौखट पर बैठा दिया जाता था, जब मैं फारिग हो जाता तो तेज आवाज लगाता-कर ली, धो दो। तब माँ, दीदी या भाइयों में से कोई पानी लेकर आता था, मुझे धुलाया जाता, तब मुझे उस मल पर चूल्हे की राख डालनी होती, माँ तसले में भरकर गॉंव के बाहर बनी कूड़ी पर डालकर आती। इस फारिग होने की बात और तरीके से मुझे आत्मग्लानि होती, अधिक चल-फिर न पाने के कारण कोई और चारा भी नहीं था, इस तरह फारिग होने में शर्मिंदगी महसूस होती, इसलिए कितनी ही बार प्राकृतिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास भी किया। कोशिश होती कि जब रात हो जाए और गली से लोगो का आना-जाना बन्द हो जाये तो ही फारिग हुआ जाए। मैं सोचता- अँधेरे में फारिग होने जाऊँगा तो दोस्तों को पता नहीं चलेगा, पास-पडोसी को पता नहीं लगेगा, आते-जाते लोगों को नहीं दिख पाउँगा, लेकिन कोई न कोई आ ही जाता। बसंती दादी का घर हमारे घर और दुबारी के बीच होने के चलते, मेरे फारिग होने से दादी के परिवार वाले भी मुझे कितनी ही बार हिकारत से देखते- मानो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे इस बात से भी अपराधबोध होता।
सातवीं क्लास में था जब घर में फ्लश बना लेकिन उसमें बैठकर फारिग होना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता, फर्श पर उकडू बैठना मेरे लिए संभव नहीं था- पीछे अपने दोनों हाथ टिकाकर ही फारिग होना पड़ता, अब बड़ा होने का अहसास होने के चलते मैं धोने के लिए किसी को आवाज नहीं लगाता, बस जैसे-तैसे खुद ही धोने की कोशिश करता, फ्लस बनने से जितना शुकून मुझे मिला, उससे कहीं अधिक बसंती दादी के परिवार को भी मिला, अब उनकी हिकारत दृष्टि जो खत्म हो गयी थी, और माँ को भी राहत मिली-अब उसे तसले में वह सब भरकर कूड़ी तक फेंकना नहीं था।
आधा मकान जो पहले कच्चा था वह अब पक्का हो गया था। दुबारी वाला हिस्सा बसंती दादी को देकर उनका कुछ हिस्सा बदले में लिया गया, तब ही फ्लश बनना सम्भव हुआ। अब पूरा मकान पक्का था लेकिन अभी उसकी जमीन कच्ची ही थी, बरसात में फिसलन होने या काई जमने से कितनी ही बार उस पर फिसला, तब घुटनों में बहुत चोट लगती, घुटने छिलने से चलने-फिरने में कष्ट होता, फिर जिन्हें ठीक होने में पंद्रह-बीस दिन लगते, कभी तो ये अवधि बढ़कर महीने से भी ज्यादा हो जाती, घुटने सूज भी जाते, ऐसे में कोई दवा भी लगाना मुश्किल होता।
इन कष्टों को सिर्फ वह जानता है, जिसने भोगा है, यहाँ सांत्वना बहुत मायने नहीं रखती, शायद मेरे लिए भी सांत्वनाओं का ज्यादा मोल कभी नहीं रहा। कुछ जीवन के बाद शायद इन कष्टों के साथ ही सहज होना सीख लिया।