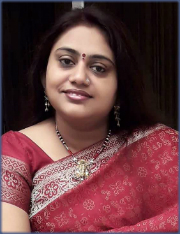लेख
चिपको की जरूरत ही क्यूँ कर पड़े
– प्रीति राघव प्रीत
बचपन की कच्ची उम्र से ही पेड़-पौधों से बहुत लगाव रहा मेरा। सही उम्र तो याद नहीं पर इतनी थी कि किसी अर्दली के संग पुलिसलाइन और बटालियन के दोस्तों के घर तक भेज दिया जाता था। और सबसे करीबी दोस्तों में से एक घर था कमांडेंट गुरदयाल सिंह गिल जी का बंगला। इतना बड़ा बगीचा कि प्रीत की उस सफ़ेद सूती फ्रॉक, जिस पर नारंगी गुलाबों का बारीक प्रिंट था; उस की ओली में न समाये। पहुँचती तो थी उनके बगीचे में नहा धोकर लेकिन वापिस सिर से पैर तक मिट्टी में लिपी-पुती ही आती थी और अम्मा की डाँट के बाद फिर से नहाना होता था। हाँलाकि बगीचा हमारे बंगले पर भी था मगर दूसरे के बगीचे के फल अधिक मीठे और मिट्टी ज्यादा सौंधी जो लगती है।
एक डी. एफ. के सिपाही थे- शिवप्रताप, जिन्हें मैं आज तक दद्दा बोलती हूँ। वो बटालियन से रोज़ाना मेरे लिये ख़ाकी लिफाफे में रखकर मोटे ताजे गुलाब के फूल लाया करते। बड़ी ख़ुश होती थी तब छुटपन में। शनैः-शनैः जब बड़ी होने लगी तो ख़ुद अपने हाथों हर नये बंगले में पौधे रोपने, सींचने लगी और जब बाबा के ट्रांसफर के बाद भी उन मेरे लगाये पेड़ों के फल हमारे घर तक भेजे गये, तो वो ख़ुशी और ख़ुशबू उनसे कहीं ज्यादा कीमती और मनबसिया साबित हुई, जो दद्दा के लाये उन गुलाबों में थी। और तब किशोरावस्था में बीज पड़ा मेरे भीतर कि फूल-पत्ते तोड़ो मत वरन् और लगाओ।
ये महज़ देखने से मन हरा नहीं करते बल्कि ये बहुत बड़ी जीव-जन्तु, पक्षी, कीटों की संख्या का आश्रय हैं, नीड़ हैं, भोजन हैं, छाया, हवा, श्वाँस, जीवन हैं। यही नहीं ये व्यवसायिक इकाई, दवाईयाँ, रोज़ी-रोटी क्या कुछ नहीं हैं ये पेड़-पौधे।
इसी प्रेम के कारण विषय लिया था बॉटनी और आज कृषक तो नहीं हूँ पर अधिकतर पेड़-पौधों के बाबत् सब जानकारी रखती हूँ। और बस तब से यही कोशिश रही कि बेटी को भी उगाना सिखाऊँ, ध्वस्त करना, तोड़ना नहीं।
उसे भी तोड़ने नहीं दिये फूल-पत्ते बल्कि यही सिखाया कि लगाओ और बढ़ाओ इस हरित जीवन को। इन्हीं से हमें प्राणवायु मिलती है।
किशोरावस्था से लेकर आज दिन तक पेड़ों की और हरितक्रांति की जब भी कोई बात निकलती है तब एक अति विशिष्ट और अनोखी क्रांति मन में कुछ बीज रोप जाती है। ‘चिपको आंदोलन’ यही वो अहिंसक क्रांति थी, जो कि वनों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये की गयी थी। यह आंदोलन व्यवसाय हेतु वनों की कटाई के विरोध में शुरू हुआ, जिसमें उत्तराखण्ड की ग्रामीण पहाड़ी महिलाएँ वृक्षों से लिपटकर खड़ी हो गयीं, जिससे वो काटे न जा सकें। उन निडर व साहसी महिलाओं ने सबको ये सिखा दिया कि वो जननी हैं इसलिये माँ प्रकृति की पीड़ा भली-भाँति समझती है। यह चिंतालिप्त आलिंगन प्रकृति से मनुष्य प्रेम का प्रतीक बन गया। चिपको आंदोलन पारिस्थितिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर हरित् वन्य जीवन की जद्दोजहद और जीत बनकर इतिहास में दर्ज हुआ।
चिपको की शुरूआत असल में 26 मार्च, 1974 को उत्तरप्रदेश (वर्तमान में उत्तराखंड) के चमोली जिले के रैंणी गाँव से हुई, जो कि भारत-तिब्बत सीमा पर जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा और विष्णुगंगा के संगम पर बसा है। वन विभाग ने इस क्षेत्र के अंगू के 2451 पेड़ साइमंड कंपनी को ठेके पर दिये थे। इसकी ख़बर मिलते ही ‘चंडी प्रसाद भट्ट’ के नेतृत्व में 14 फरवरी, 1974 को एक सभा की गई, जिसमें लोगों को चेताया गया कि यदि पेड़ गिराये गये तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। ये पेड़ न सिर्फ हमारी चारे, जलावन और जड़ी-बूटियों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, बल्कि मिट्टी का क्षरण भी रोकते है, जिसके कारण हमारे पहाड़ी इलाके सुरक्षित हैं। वनों व वृक्षों की कटाई मृदा अपरदन को बढ़ावा देगी।
इस सभा के बाद 15 मार्च को गाँव वालों ने और 24 मार्च को विद्यार्थियों ने रैणीं जंगल की कटाई के विरोध में जुलूस निकाला। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो ठीक उसी वक़्त सरकार ने एक सोची-समझी चाल के तहत घोषणा की कि चमोली में सेना के लिए जिन लोगों के खेतों को अधिग्रहण किया गया था, वे अपना मुआवजा ले जाएँ। गाँव के पुरूष मुआवजा लेने चमोली हेडक्वार्टर चले गए। दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए जिला मुख्यालय, गोपेश्वर बुला लिया। इसी मौके का लाभ उठाकर ठेकेदार और वन अधिकारी जंगलों में घुस गये। पुरुषों के चले जाने के बाद अब गाँव में सिर्फ महिलाएँ ही बची थीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिना जान की परवाह किये 27 औरतों ने ‘श्रीमती गौरादेवी’ के नेतृत्व में ‘चिपको-आंदोलन’ शुरू कर दिया।
उस समय जब मौजूदा सरकार और ठेकेदारों के कान पर जूँ भी न रेंगी तो वे महिलाएँ कटाई प्रक्रिया के समय पेड़ों से लिपट गयीं, इस ललकार के साथ कि ‘पहले हमें काटो, फिर पेड़ों को’! उनकी ये ललकार इतनी साहसी और दृणनिश्चयी थी कि ठेकेदारों और सरकार को पीछे हटकर हथियार डालने पड़े। रैंणी गाँव का जंगल बच गया कटाई से। इस आंदोलन की असली विजय तब हुई जब कि 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर पंद्रह साल के लिये रोक लगा दी। धीरे-धीरे इस आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव के कारण ये उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और तदुपरांत मध्य भारत में विंध्य तक फैला भी और सफल भी रहा। यह आंदोलन लोगों को प्राकृतिक आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति सचेत व सजग बनाने में तथा ‘प्राकृतिक संसाधन नीति’ के प्रति जागरुकता लाने में मील का पत्थर साबित हुआ। दूर-दराज के शहरों-गाँवो में चिपको का संदेश पहुँचाने के लिए विभिन्न पद्वतियों का सहारा लिया गया, जिनमें प्रमुख थे- पदयात्राएँ, लोकगीत तथा कहानियाँ आदि। लोकगायकों ने उत्तेजित करने वाले गीत गाये। नारे बनाये और लगाये गये-
‘क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार।
मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार।”
इस प्रकार 26 मार्च, 1974 को स्वतंत्र भारत के ‘प्रथम पर्यावरण रक्षक आंदोलन’ की नींव रखी गई।
इस अद्भुत आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात रही महिलाओं के द्वारा बड़ी मात्रा में एकजुट होकर, निडर बने रहकर इसका जयघोष करना- ‘ये जंगल हमारा मायका है, इसे हम कटने नहीं देंगे।’– जो कि अपने आप में ‘नारी सशक्तिकरण’ का सार्थक उदाहरण है। महिलाओं ने चौका-चूल्हा के गृहस्थी प्रेम के संग अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और प्रकृति से प्रेम को अमर बना दिया। वैसे ‘मायका मतलब माई का घर’ हर महिला के लिए वह सुखद स्थान है, जहाँ वे किसी भी संकट के समय में भी सुरक्षित रहती हैं। बचपन से वो मायका खुशियों, शिकायतों, मनमर्जियों, ज़रूरी सीखों व जीवन-पाठों का आश्रयदाता होता है।
वास्तव में पहाड़ी महिलाओं और जंगलों का अटूट संबंध है। पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी के बहकर चले जाने से रोज़गार के लिए पुरुषों के पलायन के फलस्वरूप गृहस्थी का सारा भार महिलाओं पर ही पड़ता है। पशुओं के लिए घास, चारा, रसोई के लिए ईंधन और पानी का प्रबंध करना खेती के अलावा उनका मुख्य कार्य है। महिलाओं का वनों से सीधा संबंध है। वनों की व्यापारिक दोहन की नीति ने घास-चारा देने वाले चौड़ी पत्तियों के पेड़ों को समाप्त कर चीड़, देवदार के शंकुधारी धरती को सूखा बना देने वाले पेड़ों का विस्तार किया है। मोटर-गाड़ियों, सडक़ों के विस्तार से होने वाले वनों, पेड़ों के कटाव के कारण रसोई के लिए ईंधन का अभाव होता है। इन सबका भार महिलाओं पर ही पड़ता है। अत: इस विनाशलीला को रोकने की चिंता वनों से प्रत्यक्ष जुड़ी महिलाओं के अलावा और कौन कर सकता है। वे जानती हैं कि मिट्टी के बहकर जाने से तथा भूमि के अन-उपजाऊ होने से पुरुषों को रोज़गार के लिए शहरों में जाना पड़ेगा। पेड़ होंगे तो उनकी जड़ों से मिट्टी रुकेगी तो खेती का आधार मजबूत होगा। पुरुष घर पर टिकेंगे। इसका एक मात्र उपाय है- हरे पेड़ों की रक्षा करना क्योंकि पेड़ मिट्टी को थामने का जरिया हैं। इनके रहने पर वर्षा भी अपने रास्ते नहीं बदलेगी।
दरअसल चिपको आंदोलन को प्राय: एक महिला संचालित आंदोलन के रूप में ही जाना जाता है क्योंकि इसकी अधिकांश कार्यकर्ता महिलाएँ ही थीं। चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वनों के प्रबंधन में अपनी भागीदारी की माँग भी की। उनका तर्क था कि वह औरत ही है जो ईंधन, चारे, पानी आदि को एकत्रित करती हैं। उसके लिए जंगल का प्रश्न उसकी जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। अत: वनों से संबंधित किसी भी निणर्य में उनकी राय को शामिल करनी चाहिए। चिपको आंदोलन ने वंदना शिवा जी को विकास के एक नये सिद्धांत- ‘पर्यावरण नारीवाद’ के लिए प्रेरणा दी, जिसमें पर्यावरण तथा नारी के बीच अटूट संबंधों को दर्शाया गया है।
मेरा यह सब कहने का मकसद महज़ इसलिये नहीं कि विश्व पर्यावरण दिवस के माह में कोई भागेदारी भर दर्ज करनी है। बल्कि ये आज मैं याद दिला रही हूँ आप सबको हमारा वो बल जिसमें भुजाओं की ताकत नहीं बल्कि रुधिर कोशिकाओं में बहते जज़्बे और निडरता की रव़ानी है।
आज हमारे ही शहरों के लाइफस्टाइल ने हमारे पर्यावरण को क्षरण के गर्त में धकेल दिया है। हम अपनी ही उगाई नेमतों को नष्ट कर के किसी विकास की ओर नहीं वरन् विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई ने मानसून व वर्षाचक्र बिगाड़ दिया है। शहरीकरण व विकास के नाम पर लगातार जमीन को खोखला करने की प्रक्रिया ने भूकम्पों की दरों में बढ़ोत्तरी कर दी है।
ग्लोबल वार्मिंग के किनारे पर खड़े हम बस तमाशबीन बने हुए हैं अपनी ही बरबादी के। लगातार दुनियाभर के पर्यावरणविदों और संस्थानों द्वारा दी जाने वाली चेतावनी को कितना हल्का समझ रहे हैं हम। हमारे फैलाये क्लोरो-फ्लोरो कार्बन के द्वारा हमारी ओज़ोन की सुरक्षा परत क्षय कर रही है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा और विनाशकारी विकिरण धरती तक अपनी पहुँच बना चुके हैं। प्लास्टिक ने मानो हमारे मन को भी वैसा ही प्राणवायु विहीन कर दिया है। मौसमों का घटता-बढ़ता क्रम, तेजी से मौसम की परिस्थितियों में बदलाव ये सब हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। और निश्चित ही इसके जिम्मेदार हम स्वयं ही कहलायेंगे। हमारी ही स्वार्थी सोच ने पारिस्थितिकी तंत्रों के अनुपात बिगाड़ दिये हैं। हमने अपने आलीशान आश्रयों व सुविधाओं के लालच में जंगली जीव-जन्तुओं के ही आश्रय छीन लिये हैं। हमें अभी होश ही नहीं कि हमारे किये कर्मों के कितने दुष्परिणाम हमारी भावी पीढ़ी को भुगतने होंगे। हमारे स्वार्थ और प्रकृति प्रदत्त सुखों के दुरुपयोग ने आज जल का स्तर बहुत नीचे पहुँचा दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब भारत में भी ‘जीरो-डे’ के आने में ज्यादा देर बची है।
हम शहरीकरण के चलते बस पेड़ों, वनों, खेतों, बगीचों, तालों आदि को नष्ट करते, काटते, सुखाते जा रहे हैं। जमीनें ख़ुद ही मशीनों द्वारा खोखली करे जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी करे जा रहे हैं।
जबकि आज हमारा हरा-भरा इतिहास ही हमें एक जज़्बा दे रहा है संगठित होकर अपने पर्यावरण की प्राकृतिक संसाधनों की और माँ प्रकृति की रक्षा हेतु। हमारा वर्तमान हमें चेतावनी दे रहा है भविष्य में होने वाली भीषण प्राकृतिक आपदाओं की।
क्या पूछ सकती हूँ एक सवाल महिला होकर महिलाओं से कि जब कम पढ़ीलिखी ,चौके-चूल्हे में लिप्त ग्रामीण महिलायें अपने पर्यावरण की रक्षा हेतु एक क्रांति का विजयघोष कर सकती हैं तो क्या हम शहरी तौर-तरीकों,शिक्षा व सहूलियतों से परिपूर्ण और प्रख़र महिलायें किसी भी लायक नहीं हैं?
इतने लाखों के खर्चों में संलग्न होकर हम आलीशान, मनचाहे मकानों को बनाते में हम क्यूँ नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रक्रिया को निर्मित कराते? क्यूँ नहीं हम सबको आगाह करते कि हम जुड़े हैं सोशल मीडिया के जरिये हर कहीं? तो क्यों नहीं हम अपने ज्ञान का, शिक्षा का सदुपयोग करते? तो क्यूँ नहीं हम अपना समय व्यर्थ की दिखावागिरी से समेट कर प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण की रक्षा की जागरूकता हेतु खर्च करते? कहाँ पाते हैं आज हम ख़ुद को उन चिपको आंदोलनकारी महिलाओं के सम्मुख?
पहचानिये अपनी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सशक्त ऊर्जा को और शुरूआत करिये इसी माह से इसी क्षण से बूँद-बूँद से घट भरने की।
किसी सार्थक, अहिंसक, शांत क्रांति के लिये भला कब हथियारों और चौराहों, चबूतरों या रणभूमि की आवश्यकता ठहरी है। हम घर से बाहर निकलकर शुरुआत अपने अड़ोस-पड़ोस, गली, मौहल्ले और शहर, गाँव, कस्बे से तो कर ही सकते हैं, नहीं क्या?
मेरी प्रेरणा ‘गौरा देवी से लेकर वरिष्ठ लेखिका चित्रा देसाई जी’ तक वो सभी हैं, जो अपनी प्रकृति, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिये हर संभव मोर्चा संभालती हैं और उसमें अपने भीतर की अंतर्शक्ति को समेट कर स्वयं ही एकला चलो रे की थाप पर विजय का नेतृत्व करती हैं। तो फिर उठिये और लगाईये वृक्ष और बनिये हजारों कलरवों की चहक, भोजन व आश्रय की वजह। घर पर पोर्च और गाड़ियों की धुलाई का पानी बचाकर दीजिये अपने मोहल्ले के किसी सूखते पेड़ में पानी। उसकी हरी पत्तियाँ…आपको देखकर अनुराग से भर उठेंगी।
चिपको की जरूरत ही क्यूँ कर पड़े कि हम ही ठान लें कि बीज रोपेंगे, पानी सींचेंगे और उगायेंगे प्रकृति से पर्यावरण से अपना प्रेम का रिश्ता और बनेंगे मिसाल प्रकृति के प्रेमी बनकर। तो चलें फिर आज शाम की वॉक पर निगाह में गणना करने कि कहाँ कोई हरियल पेड़-पौधा दम तोड़ रहा है। मुहिम चलाने को बस सकारात्मक नियत ही काफ़ी है।
– प्रीति राघव प्रीत