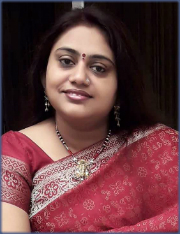समय भले ही बदला हो या हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो गए हो मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा समाज आज भी पितृसत्ता की अगुवाई करता है। कुछ अनुपात में पीढियों के विचार उनकी मानसिकता भी भले ही बदली हो मगर जड़ों में बैठी सोच उस जमाने से इस जमाने तक आज भी वही की वही है।
महल हो, विला-बंगले हों, कच्चे-पक्के मकान हों या झोंपड़ी ही क्यों ना हो…दो जुमले इन सबकी नींव में हर युग में चिनवा दिए जाते रहे हैं कि-‘मर्द रोते नहीं’…’मर्द को दर्द नहीं होता!’
क्यूँ नहीं रोते? क्या उनकी आँखों में अश्रु ग्रंथियाँ नहीं होतीं या फिर उन्हें दिल बस काँच के शो-पीस के रूप में मिला है, जिसमें कोई भी संवेदना किसी तरह की उथलपुथल नहीं मचा सकती?या फिर उन्हें कोई ऐसा श्राप लगा है कि-आँसू टपकते ही वे सब स्त्री रूप में बदल जायेंगे? वे भी सजीव हैं तो दर्द क्यूँ नहीं हो सकता उन्हें?या फिर वे सभी लौह के बने हैं या उनके हाड़-माँस की जगह पाषाण भरे हुए हैं?
कहते हैं किसी भी बालक की पहली पाठशाला उसका घर-परिवार होता है और माता-पिता उसके प्रथम शिक्षक। यदि नीड़ का निर्माण करते शिक्षक ही उस नीड़ में वायु के लिये आवश्यक छिद्र नहीं छोड़ेंगे तो वह तो दमघोंटू ही बन जायेगा ना! आज के माहौल को देखते हुए पाठ्यक्रम के नवीनीकरण की महती आवश्यकता है। हमें वीरता के पाठ से पहले उन्हें संवेदना का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। ये पाठ भी पढ़ायें कि घर-परिवार की स्त्रियों के सम्मान के साथ-साथ परस्त्री का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। स्वहित से पहले राष्ट्रहित हो, घर निर्माण से पहले चरित्र निर्माण और स्त्री व पुरुष से पहले मनुष्यता, दया, करुणा हो।
हमें बहुत छोटी सी बात समझनी अत्यावश्यक है कि- भेद सदा से ही बाँटते आये हैं। तो जो बाँट कर विभाजित कर दे ऐसी मानसिकता के बीज बाल्यकाल की कच्ची मिट्टी में बोने ही क्यूँ हैं?
कबीर दास जी तो कब से आसान शब्दों में समझा गये हैं-
“गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ि-गढ़ि काढ़ै खोट।
अन्तर हाथ सहार दै, बाहर मारै चोट॥
आज के समय में पुरुष मन के भीतर पनपते तनाव, डिप्रेशन, आइशोलेशन को संवेदनात्मक सधे हाथों के सहारे की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि अति सदा ही भयावह होती है इसी कारण पिता, पुत्र, पति, प्रेमी बनता पुरुष ही संवेदना से विलग वीरता का बोझ जब संभाल नहीं पाता तब दंभ से परिपूर्ण बीमार मानसिकता का उदय होता है। (कुछ अपवादों में यही घमंड सिर चढ़ जाता है तब वहाँ वीभत्स, विकृत कुंठा तक पनप जाती है, जिसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं।)वह घर से शगुन में मिली उस वीरता के मद में चूर होने लगता है और तब प्रारंभ होता है शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का थरथरा देने वाला दौर। इस प्रताड़ना की टीस भोगता है भेद के खाँचे का आधा हिस्सा यानि आधी आबादी। ऐसे में क्या दोषारोपण उस एक पुरुष खाँचे पर मढ़ देना उचित है?
निपट आश्चर्य की बात है कि जब बालक के प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षक अर्थात् माता-पिता उस बालक को भेद की सारणी बनाकर नहीं बल्कि एक इकाई की तरह संगठित होकर ही जीवन के पाठ पढ़ा रहे थे!तब कैसे उस पाठ में भेद की रेखा खिंच गई या मैं समझूँ कि..जानबूझकर खींच दी गई? किसके द्वारा खींच दी गई? क्यूँ घर-परिवार के लिए और समाज के लिए नियमों में भिन्न-भिन्न कायदे-कानूनों के अनुपातों को रख दिया गया? कैसे उसे अपने मर्द होने पर घमंड होने लगा? कैसे वह संवेदनाओं को महसूस करना भूल गया? कैसे कोमल बालक एक हिंसक, रूखा, बे-दिल पुरुष बन गया?
या फिर क्यूँ कर वह गुमसुम, घुन्ना या तमाम असाध्य रोगों का अड्डा बन गया?
सोचा है कभी आपने?
बालक के कदम घर की चौखट के बाहर निकलने से पहले सोचने और समझने की सबसे अधिक आवश्यकता है हर उस स्त्री को, जो चौखट के भीतर उस बालक के जीवन का अभिन्न अंग होती हैं।
अक्सर ही आस-पडोस, जान-पहचान, रिश्तेदारियों में देखा सुना है कि पुरुषों के अनुपात में कहीं अधिक घर की महिलाएँ ही मासूम बचपन को लौह-पुरुष में बदलने में पूरी आस्था से प्रयासरत रहती हैं। बालक खेलते हुए गिरा या भाई-बहिनों या दोस्तों से पिटा तो …’तू लड़का होकर कैसे पिट आया?’, ‘लड़के यूँ लड़कियों की ताईं ना रोते।’, ‘तू तो घणां वीर है दो-चार ने मार कै आऊगा।’, ‘लड़की हो के उसकी इतनी हिम्मत?दो लगा कान के नीचे।’, ‘तू तो शेर बच्चा है।’, ‘जनानियों की तरह नाजुक ना बन छोरे।’
कितने ही वाक्य जो खदकती चीनी को तपाते जाते हैं साल दर साल और व्यवहार की चाशनी एक तार, दो तार, तीन तार की होते-होते शक्कर का कठोर ढिम्बा बन जाती है।
हमारे समाज में कंडीशनिंग के जो नियम-कायदे हैं वो एक हृदय को बिना आहट ना जाने कब रूखा और कड़ा बना देते हैं, यह पता तक नहीं चलता। या जब आपके ही द्वारा पोषित पौधा जब काँटेदार वृक्ष बनकर आपको खरौंच देता है तब आपको भान होता है, लेकिन समझने व सुधारने में बहुत देर हो चुकी होती है।
किसी भी कोमलमना बालक को संवेदनशील व्यवहार के चलते हर घर, पडोस, स्कूल-कॉलेज में सरकाज्म से भरे ताने मिलते हैं। लड़का यदि ओवर सेंसिटिव या ओवर प्रोटेक्टिव है, एक्स्ट्रा पोलाइट है तो साथ पढ़ती लड़कियाँ भी सहपाठियों के संग उसको बुली करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं।
मुझे याद है जब हम आठवीं कक्षा में थे, तब एक प्यारा सा लड़का क्लास में आया(नाम नहीं लिखूँगी), उसके पिता हमारे शहर में ट्राँसफर होकर आऐ थे। वह बहुत कोमलमना लड़का था, मीठी बोली, मृदु व्यवहार, सलीकेदार, दूसरों की तकलीफों को महसूस करने वाला। हमारे यहाँ के सहपाठी लड़कों ने पहले उसे बुली करना शुरू किया, फिर धीरे-धीरे कुछ लड़कियों ने भी उसकी खिल्ली उडाई। नतीजतन मुस्कुराता हुआ वह चेहरा मुरझाने लगा। हर कक्षा में एक सी सोच-समझ रखने वाले मित्रों के समूह हुआ करते हैं। हमारा भी था, मेरे समूह ने उसे बिना किसी जजमेंट के अपना लिया। वह हमारे साथ अक्सर रहने लगा, हम सभी साथ लंच करते, वार्षिकोत्सव के लिए संग प्रैक्टिस करते और छुट्टी में साइकिलें लेकर साथ-साथ स्कूल से अपने-अपने घरों को निकलते थे। हमारा ग्रुप थोड़ा अलग था मतलब पढ़ने में ठीक, कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं में आगे और सबसे ज्यादा प्रधानाचार्या और दीदियों व आचार्यों का प्रिय। वह हमारे साथ रहते-रहते तानों, उदासियों से उबर आया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब बाकी लड़कों ने भी उसके प्रति हरकतें करनी छोड़ दी।
मुझे याद है कि एक बार वह बुरी तरह रो रहा था और कह रहा था कि मैं स्कूल बदलवा लूँगा, पर अब उसे स्कूल बदलने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हम सब दसवीं तक संग रहे फिर ग्यारहवीं के लिये सभी को स्कूल बदलने पड़े थे। किसी को ताने मारना, बुली करना, नीचा या छोटा दिखाने से उस बच्चे का कद कभी कम नहीं हो जाता बल्कि हम अपनी कुंठित मानसिकता को दर्शा देते हैं, हम जता देते हैं कि हम अपनी कुंठा को तृप्त कर रहे हैं।
कभी सोचा है हमने कि लड़कों का संवेदनात्मक व्यवहार जिसमें वे भी कभी किन्हीं परिस्थितियों में कई कारणों से अपनी एकांत को समेट कर रो लेना चाहते हैं, वे बहा देना चाहते हैं भीतर का इकट्ठा दर्द जो गले में एकत्र होकर जहर बनने लगता है, घोंटने लगता है उनका भी गला। चिंताओं, परेशानियों की बर्फ को पिघला कर तरल बना देना चाहते हैं!!
मैंने मेरे बहुत करीबी, आजीवन हर परिस्थिति में अंगद का पैर बने पुरुषों को बमुश्किल एक या दो बार रोते हुए नहीं बल्कि अकेले में बैठकर भीगी पलकों को पोंछते, गीली आँखें चुराते देखा है। उन्हें कम उम्र में बीमारियों का ठिया बने, घूमते देखना कष्टकारी लगता है मुझे। मगर बहुत आसान सा हल भी तो हम परिवारियों, दोस्तों, रिश्तों के हाथ में ही है! मैंने हल निकाला उनका हाथ अपने हाथ में लेकर, उन्हें अपना कंधा देकर उस पर उनका सिर टिकाकर कहा है कि रो लीजिए यदि भीतर से रुंध गये हैं तो…।
रुलाई फूटी और बह गया बहुत कुछ जो पूरी तरह खोखला कर सकता था तन और मन दोनों को।
क्या आपने कभी गौर किया है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में तीस-पैंतीस की उम्र में क्यों डायबिटीज, हायपरटेंशन, हार्ट से संबंधित घातक बीमारियाँ अपनी जड़ें मजबूत कर लेती हैं?जबकि वे तो नियमित एक्टिव रहते हैं। खान-पान भी समय पर व सही मात्रा में होता है। तब कैसे हम कह देते हैं तुरंत कि …’अरे इतनी कम उम्र में फलाँ बीमारी पाल ली?’
सोचिए ना तनिक कि हम स्त्रियाँ आपस में बोल-बतला कर, रोकर मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन पुरुष को तो हमारे समाज में बचपन से जिन्दगी के दुखड़े बाँटने या रोकर हल्का होने की सख़्त मनाही रही है।
यही नहीं इससे इतर जब यौन उत्पीड़न का राक्षस बालकों, लड़कों, पुरुषों को भी मानसिक व शारीरिक त्रास देता है, तब वे इस तकलीफ़ को भी खुलकर कभी किसी से कह नहीं पाते हैं। नतीजतन वे आजीवन कुंठा और घृणा के संग जिये जाते हैं। ऐसे जीने से उनकी पीड़ा तो कम नहीं होती बल्कि उनकी उम्र अवश्य कम हो जाती है।
सोचिये ना! करिए मनन इस बात का। अरे गोली मारिए ऐसी कठोर कंडीशनिंग को! थोड़ा रो लेने दीजिए आपके आसपास, आपसे जुड़े मर्दों, लड़कों, बालकों को…भई हाड़-माँस के बने हैं तो दर्द उनको भी होता ही होगा। आँसू उन्हें भी आते ही हैं। उनके दिल में भी अपार संवेदनाएँ भरी पड़ी हैं।
छलकने दीजिए उन्हें भी, पहचानिए उनके व्यवहार में आई तब्दीलियों को, पढ़िए उनके माथे की शिकन, उनकी आँखों का गीलापन, पकड़ कर बैठा लीजिए जबरन पूछिए कि-यदि परेशान मन में कुछ है तो बहा दें, कर दें चुगली, उगल दें भीतर का दर्द जो गुस्से का सिस्ट बनकर कभी किसी पर भी ना फूटे।
करिये ना …सच्ची बहुत अच्छा लगेगा।