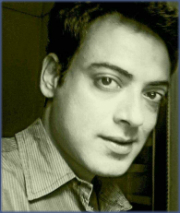नज़्म
महफ़िल से जो ऊबा तो ख़याल आया
क्यों ना कुछ वक़्त अपने साथ गुजारूं
दिलकश और दिलफ़रेब ही सही यह मुखौटे
कभी तो हिम्मत करके इन्हें उतारूँ
मुमकिन है न फिर कोई हमनवा मिले
झूठी मुस्कराहट से मिले? सनम तो क्या मिले?
पर शोख़ी फितरत की फिर भी है बरकरार
ग़मों के सैलाब आये तो हज़ारोँ बार
मैं क्या करूँ मेरी आदत है मुस्कराने की
शामिल है नहीं ख़ामी मुझमें हार जाने की
************************
नज़्म
जीने की अजब चाह है हर इक इंसान में
रंगीनियों में हो या कि बियाबान में
बस इक पल की और ज़िन्दगी दरकार है सबको
महफ़िल में हो या शहर-ए-अंजान में
घिसटता हो चाहे रोज़ फुटपाथ पर
सोया हुआ हो या महल-ए-आलीशान में
गिरकर सा संभल चुका हो या संभल कर बदल चुका
बिखरा हुआ हो या तब्दील हो चुका हैवान में
ज़िंदा है ये उतनी है हाकिम के तख़्त पर
जितनी है ये मौजूद जंग के मैदान में
कुछ और जोड़ने की चाह है के छोड़ती नहीं
मशहूर-ए-ज़माना हो या चाहे गुमनाम में
दिल है कि मौत बरहक़ मानता नहीं
गीता मैं लिखा हो या पढ़ लूँ क़ुरआन में
– एहतिशाम अज़ीज़