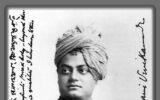भारत में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लोकतंत्र की स्थापना तक प्रेस को सूचना के चौथे स्तंभ के रूप में सम्मान मिला था। प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, पत्रकारों ने सत्ता को जवाबदेह ठहराने और जनमत को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। निष्पक्ष पत्रकारिता किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है। यह नागरिकों को सटीक, संतुलित और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे सूचित निर्णय ले सकें और सरकार को जवाबदेह ठहरा सकें।
प्रेस, आज अपनी विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है। कभी सूचना और ज्ञान का सबसे भरोसेमंद स्रोत माने जाने वाले समाचार माध्यमों पर आज सवाल उठ रहे हैं। आम जनता के मन में यह संदेह गहराता जा रहा है कि क्या वाकई प्रेस निष्पक्ष और सत्य जानकारी दे रहा है?
भारत में हाल के वर्षों में मीडिया एवं प्रेस पर भरोसा लगातार घट रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर आ गया है, जिसकी स्थिति “बहुत खराब” बताई गई है । एक अन्य सर्वे में ऑनलाइन न्यूज उपयोगकर्ताओं में कुल न्यूज पर भरोसा सिर्फ 36% पाया गया और 57% ने समाचारों की सत्यता को लेकर चिंता जताई।
आम लोग अब मीडिया की खबरों पर सहज विश्वास नहीं करते। इस गिरावट के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं – जिनमें मीडिया का पक्षपात, फेक न्यूज़, टीआरपी-दौड़ वाली सनसनीखेज कवरेज, राजनीतिक दबाव और कॉर्पोरेट स्वामित्व प्रमुख हैं।
शहरी युवा विशेष रूप से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर खबरें देखते हैं। हालांकि डिजिटल मीडिया ने सूचना जल्दी पहुँचाई है, वहीं वायरल फेक न्यूज़ की आशंका भी बढ़ी है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर एल्गोरिद्मिक बबल और सूचना की बाढ़ ने सतही खबरों को बढ़ावा दिया, जिससे डिजिटल माध्यम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं।
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ का प्रकोप मीडिया की विश्वसनीयता को और कम कर रहा है। देश में अनेक ग्रुप्स और सोशल अकाउंट्स ने गलत चित्र, वीडियो और कहानी चलाकर माहौल भुनाया है; कई बार न्यूज चैनल भी इन झूठी सूचनाओं का अंधाधुंध प्रसारण कर देते हैं।
2023 में भारतीय मीडिया ने 77 झूठी या भ्रामक ख़बरें प्रसारित कीं, जो कई प्रतिष्ठित चैनलों से जुड़ी थीं। इन रिपोर्टों में क्रिकेट मैच, चंद्रयान-3, इजरायल–फिलिस्तीन युद्ध समेत कई मुख्य मुद्दों पर गलत सूचनाएँ फैलीं। इस तरह की गलती-दर-गलती दर्शाती है कि जांच-परख की कमी में फेक न्यूज ने मीडिया की छवि धूमिल की है।
समाचार चैनल और अखबार अब निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। कई बार देखा गया है कि मीडिया संस्थान किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा के पक्ष में झुक जाते हैं। इससे उनकी रिपोर्टिंग में संतुलन नहीं रहता और दर्शकों को एकतरफा जानकारी मिलती है। पहले संपादकीय फैसले पत्रकार तय करते थे, अब वे कॉर्पोरेट मालिकों के वश हो गए हैं। परिणामस्वरूप, पहले की तरह अब गहराई से शोध कर खबरें लाने वाली पत्रकारिता कम हो गई है। सतही रिपोर्टिंग और जल्दी खबर देने की प्रवृत्ति ने पत्रकारिता की गंभीरता को कम कर दिया है।
भारत में बड़ी मीडिया संस्थाएँ उद्योगपतियों के स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट समूहों के हाथों में हैं। कई पत्रकार मानते हैं कि पूंजीपतियों का प्रभाव संपादकीय स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है। शक्तिशाली राजनेताओं और राजनीतिक दलों का भी मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ा है। कई उदाहरणों में देखा गया कि सत्तारूढ़ दल को आलोचनात्मक रिपोर्टिंग करने पर संपादकों को दबाव झेलना पड़ा या पत्रकारों को हटाया गया। हमेशा बड़े व्यापार घरानों ने मीडिया को वित्तपोषित किया, लेकिन अब नियंत्रण लगभग पूर्ण हो गया है।
विज्ञापन आय और कॉर्पोरेट फंडिंग के दबाव में चलने के कारण कई मीडिया हाउसों की रिपोर्टिंग किसी के खिलाफ आलोचना करने से कतराती दिखती है। इसके चलते जनता को लगता है कि वे जो ख़बर देख रहे हैं, वह व्यापार या सरकार की खींचतान में बनी हुई है, और इसलिए वे मीडिया पर भरोसा नहीं कर पाते।
टीवी न्यूज चैनलों में टीआरपी बढ़ाने के लिए सनसनीखेज समाचारों को तरजीह मिल रही है। हालिया संसद समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि कई चैनल अपराध और सेलिब्रिटी संबंधी खबरों को अहम मुद्दों से ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ताकि व्यूअरशिप बढ़े। दर्शक बढ़ाने की होड़ में नैतिकता की सीमाएँ टूट जाती हैं। समिति ने कहा कि कई बार मीडिया मालिकों और संपादकों के निजी हित और राजनीतिक संबंध देखे गए, जिससे पत्रकारिता की ईमानदारी प्रभावित हो रही है।
पत्रकार और मीडिया जनता की राय बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि मीडिया सरकार की नीतियों की प्रशंसा करता है, तो जनता के बीच सरकार की छवि सकारात्मक बनती है। इसके विपरीत, अगर मीडिया आलोचनात्मक हो, तो सरकार की साख को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि पत्रकार उसकी “सफलताओं” को उजागर करें और “विफलताओं” को नजरअंदाज करें।
जब पत्रकारिता पक्षपात, राजनीतिक झुकाव या व्यावसायिक हितों से मुक्त होती है, तभी वह निष्पक्ष कहलाती है। ऐसी पत्रकारिता लोगों को घटनाओं का स्पष्ट और संतुलित चित्रण देती है। जब मीडिया सच्ची, जांची-परखी और तटस्थ जानकारी प्रस्तुत करता है, तो वह जनता को मुद्दों की गहराई समझने में मदद करता है।
निष्पक्ष पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि यह समाज को दिशा देने वाली शक्ति है। यह जनमत को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसे सशक्त बनाती है। परिणामस्वरूप, नागरिक तर्कसंगत निर्णय लेते हैं — चाहे वह मतदान हो, आंदोलन हो या सामाजिक बदलाव की पहल। इसके माध्यम से जनता तथ्यों को समझकर स्वतंत्र रूप से विचार बना सकती है, न कि प्रचार और भ्रम के आधार पर।
इतिहास गवाह है कि आपातकाल (1975-77) के समय जब प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, तब जनता की सही जानकारी तक पहुंच बाधित हो गई और जनमत प्रभावित हुआ। वहीं दूसरी ओर, निर्भया कांड के समय मीडिया की मुखर और सटीक रिपोर्टिंग ने न केवल देश भर में रोष पैदा किया, बल्कि कानूनों में सुधार की मांग को भी मजबूती दी।
पत्रकारों का मुख्य कर्तव्य होता है सत्य को उजागर करना और जनता को सूचित करना। लेकिन जब पत्रकारिता सत्ता के संरक्षण में आती है, तो वह अपने उद्देश्य से भटक सकती है। जब पत्रकार सरकार या सत्ताधारी दलों से आर्थिक, वैचारिक या संस्थागत संरक्षण प्राप्त करते हैं, तो निष्पक्षता की कसौटी पर उनकी विश्वसनीयता अक्सर संदेह के घेरे में आ जाती है। ऐसे पत्रकार सत्ता के आलोचकों को “राष्ट्र विरोधी” बताने लगते हैं, जबकि जनहित से जुड़े प्रश्नों जैसे महँगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को हाशिये पर डाल दिया जाता है।
इस प्रकार की पत्रकारिता का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि एक जागरूक और सवाल पूछने वाला समाज धीरे-धीरे निष्क्रिय हो जाता है। जब जनता को सच्चाई की बजाय भ्रामक सूचना परोसी जाती है, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। सरकार की जवाबदेही घटती है और नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।
जब पत्रकार सरकार से सवाल करता है —तब वह आम नागरिक की ओर से जवाबदेही की मांग करता है। यह सवाल भ्रष्टाचार पर हो सकते हैं, नीतियों की नाकामी पर, जनकल्याण योजनाओं की हकीकत पर, या फिर आम आदमी की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर। यदि पत्रकारिता केवल सरकार की तारीफ करने का माध्यम बन जाए, तो वह “जनसेवा” से हटकर “प्रचार तंत्र” बन जाती है।
आज के समय में जब मीडिया का एक हिस्सा टीआरपी और विज्ञापन के दबाव में है, तब भी कई पत्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सत्ता से असहज सवाल पूछते हैं। यह साहस, ईमानदारी और पेशेवर निष्ठा का प्रमाण है।
पत्रकारिता का उद्देश्य यह नहीं है कि वह किसी राजनैतिक दल के लिए पक्ष या विपक्ष बने —उसका उद्देश्य है सच्चाई तक पहुँचना, जनता को सूचित करना और लोकतंत्र की रक्षा करना। एक जागरूक समाज वही है जहाँ पत्रकार स्वतंत्र हों, निर्भीक हों और सत्ताधारियों से प्रश्न पूछने की आज़ादी रखते हों।
पत्रकार का काम है सच को उजागर करना, सत्ता से सवाल पूछना और आम आदमी की आवाज़ को मंच देना। लेकिन जब पत्रकार लालच, डर या सत्ता के प्रभाव में आकर सच से मुँह मोड़ लेता है, तो उसकी रिपोर्टिंग एकतरफा, झूठी या तोड़ी-मरोड़ी हुई हो जाती है। कई बार सरकार की योजनाओं का प्रभाव धरातल पर नहीं पहुंचता, लेकिन मीडिया के माध्यम से उसकी बड़ी-बड़ी उपलब्धियां दिखाई जाती हैं। यह एक तरह की ‘इमेज मैनेजमेंट’ होती है, जिसमें पत्रकारों का सहयोग जरूरी होता है।
सरकार समर्थित पत्रकार अक्सर चुनिंदा मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, विरोध के स्वरों को दबाते हैं, और विपक्षी नेताओं या आंदोलनों को बदनाम करने में संलग्न रहते हैं। इसके लिए वे सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल, अखबारों और ऑनलाइन पोर्टलों का उपयोग करते हैं। ऐसे पत्रकार अपनी विश्वसनीयता खोते हैं और उनकी खबरें सिर्फ भीड़ को भड़काने का माध्यम बन जाती हैं।
भीड़ सोचती नहीं है। वह बस उत्तेजित होती है। जब पत्रकार अपने लेखन या रिपोर्टिंग में पक्षपात करता है, या अंधभक्ति को बढ़ावा देता है, तो वह सोचने-समझने वाले नागरिकों को उकसाई हुई भीड़ में बदल देता है। यह भीड़ न सत्य की परवाह करती है, न न्याय की —वह बस नफरत, अफवाह और प्रचार का शिकार हो जाती है।
जब पत्रकार बिक जाता है, तो समाज का दर्पण धुंधला हो जाता है। उसकी रिपोर्टिंग न सच को उजागर करती है, न झूठ को चुनौती देती है। ऐसी पत्रकारिता न सोचने वाले नागरिकों को जन्म देती है, बल्कि एक ऐसी भीड़ को खड़ा करती है जो सिर्फ़ उकसावे और भ्रम में जीती है। हमें तय करना है —हम जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं या सिर्फ एक ‘मरी हुई भीड़’ का हिस्सा?
यदि पत्रकार सरकार के बजाय विपक्ष की आलोचनाओं को प्रमुखता दें, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके उलट, जब पत्रकार विपक्ष को ही सवालों के घेरे में लाते हैं, तो सरकार को राहत मिलती है। इसलिए सरकारें चाहती हैं कि पत्रकार विपक्ष की आलोचना करें और अपनी कमियों को नजरअंदाज करें।
सरकारें अक्सर पत्रकारों को सरकारी विज्ञापन, विभिन्न पुरस्कार या अन्य सुविधाओं के जरिए अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती हैं। कुछ पत्रकारों को सरकारी समितियों में नियुक्त किया जाता है या ‘फेवर्ड’ एक्सेस दिया जाता है। इसका उद्देश्य पत्रकारों को ‘सरकारी प्रचारक’ में बदल देना होता है।
निष्पक्ष पत्रकारिता सरकारों की नीतियों, कार्यों और निर्णयों पर निष्पक्ष रूप से सवाल उठाती है। यह उन कमियों और गलतियों को उजागर करती है जिन्हें सरकारें छिपाना चाहती हैं। अगर मीडिया अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना बंद कर दे, तो जनता सूचनाओं के अंधेरे में चली जाएगी। ज़रूरत है कि मीडिया अपने दायित्व को समझे, और जनता भी सतर्क रहकर स्रोतों की पुष्टि करे। पाठकों और दर्शकों को खुद भी सवाल करना होगा कि वे जो देख रहे हैं, वह सच है या सिर्फ़ सनसनी।
पत्रकारों का उद्देश्य यदि जनसेवा के स्थान पर सत्ता की सेवा बन जाए, तो यह एक गहरी चिंता का विषय है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछता है, तो वह दरअसल हमारे ही हक़ और भविष्य की रक्षा कर रहा होता है।
निष्पक्ष पत्रकारिता सरकारों की नीतियों, कार्यों और निर्णयों पर निष्पक्ष रूप से सवाल उठाती है। यह उन कमियों और गलतियों को उजागर करती है जिन्हें सरकारें छिपाना चाहती हैं। अगर मीडिया अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना बंद कर दे, तो जनता सूचनाओं के अंधेरे में चली जाएगी। ज़रूरत है कि मीडिया अपने दायित्व को समझे, और जनता भी सतर्क रहकर स्रोतों की पुष्टि करे।
जब खबरें पक्षपाती होती हैं, तो जनता तक सच्चाई नहीं पहुँचती। इससे समाज में भ्रम, ध्रुवीकरण और अविश्वास फैलता है। लोग सोचते हैं कि जो टीवी या अखबार में आ रहा है वही सच है, जबकि वह सच्चाई नहीं, किसी खास उद्देश्य से गढ़ी गई कथा होती है। जनता को जागरूक रहना होगा, क्योंकि खबर केवल जानकारी नहीं देती—वह नजरिया भी गढ़ती है।