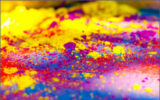आये दिन फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पर पुस्तक विमोचन की ख़बरें छपती रहती हैं, तस्वीरें, फूल-मालाएँ, बधाई और शुभकामनाओं की ताबड़तोड़ भरमार से हम सब भलीभांति परिचित हैं। उसके बाद समीक्षा और आलोचना का अंतहीन सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है। इन साइट्स से उन लेखकों को निश्चित रूप से लाभ हुआ है जो वर्षों से लिखते तो आ रहे हैं लेकिन अपनी कोई पहचान न बना सके। पुरुष अपनी नौकरी के चलते और महिलाएं घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच उतना समय नहीं निकाल पातीं लेकिन अब इंटरनेट के जरिये जनमानस तक पहुंचना अत्यन्त सुलभ हो गया है।
लेखन, एक आत्मिक संतुष्टि देता है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति का बेहतरीन माध्यम है ये। लेकिन क्या हर ‘लिखा हुआ’ साहित्य ही होता है? या कि ‘प्रकाशित’ हो जाना भर ही लेखन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है? रचनाओं की चोरी से लेकर उन्हें अपने नाम से छपवा लेने की मानसिकता किस तरह के साहित्य और साहित्यकार की ओर इंगित कर रही है? इस तथ्य से तो हम भलीभांति परिचित हैं कि इस पेशे में न तो उतना नाम है न पैसा! फिर ऐसा क्या है जो किसी को इस हद तक गिरने के लिए बाध्य कर देता है?
हर माह एक नया किस्सा होता है, जिसमें फेक आई डी और ब्लैकमेलिंग का जिक्र रहता है। कहीं कोई अपने नाम के दम पर किसी को छपवाने के दम्भ में डूबता नजर आता है तो कोई अपने गुट को रेवड़ी की तरह पुरस्कार बांटते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार घोषित कर देता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आप वर्षों से जिस क्षेत्र को सम्मान के साथ देखते आये हैं, उसकी कलई इससे जुड़ जाने के बाद ही खुलती है। लोग आपको उस हद तक गिराने के लिए तैयार हैं, जिस हद तक आप गिर सकते हैं। दोषी दोनों ही पक्ष हैं, पुरुष मदद के नाम पर देह की अभिलाषा रखता है और महिला उसे समर्पण का नाम दे देती है। काम निकल जाने पर ‘स्क्रीन शॉट’ और आरोप-प्रत्यारोप का घिनौना रूप न सिर्फ आपका मन वितृष्णा से भर देता है बल्कि आप बार-बार आँखें फाड़कर देखते हुए भी विश्वास नहीं कर पाते कि इस तरह की कोई चर्चा साहित्यकारों के सन्दर्भ में हो रही है। कितना सच, कितना झूठ, ये तो वही जाने जिस पर बीती है लेकिन यह होता है इससे इंकार नहीं किया जा सकता।
दुनिया चाहे जो भी कहे, पर एक सच ये भी है कि अपनी क्षमता और लेखनी के स्तर का अंदाज़ा हर रचनाकार को होता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। “तुम मुझे कविता दो, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा”, की तर्ज़ पर पत्रिका के हर अंक पर बँटते पुरस्कारों के क्या मायने हैं, ये पाने वाले को भी पता होते हैं। कई ग्रुप्स में भी इनकी प्रथा चल पड़ी है और जीतने वाला स्वयं को सदी का सबसे बड़ा साहित्यकार समझने लगता है। मैं उनकी रचनात्मकता पर प्रश्न नहीं कर रही, बात खुद को श्रेष्ठ साबित करवाने की है। तात्पर्य यह है कि मात्र फेसबुक पर लिखते हुए ही कोई कवि नहीं होता। ‘हिंदी साहित्य के इतिहास’ के स्वर्णिम पन्नों को पलटते ही सबकी आँखें खुल जाने वाली हैं।
इस सबमें अगर किसी का नुकसान है तो वो सच्चे और ईमानदार लेखकों का है, जिनका गुटबाजी से कोई लेना-देना नहीं, जिन्हें चाटुकारिता आती नहीं और जो सत्य को सत्य की ही तरह पेश करते हैं। क्या मेहनत और सच्चाई की राह पर आगे बढ़ते रहना गलत है? क्या सामाजिक सरोकारों पर लेखन नहीं होना चाहिए? जो छप रहा है क्या ये वही ‘साहित्य’ है जिसे हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहेंगे? आखिर इस तरह के लेखन की उम्र कितनी है? जो वर्षों से लिखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि ये दौर ज्यादा चलने वाला नहीं परन्तु किसी अच्छे रचनाकार को कुंठित देखते हुए बहुत बुरा लगता है। उसके शब्दों की तल्ख़ी, उसके भीतर की कड़वाहट का जीता-जागता दस्तावेज है। डर है कहीं पुस्तक, विमोचन, महाकुंभ और रंगीन तस्वीरों की चकाचौंध में असल साहित्य का दम न घुटने लगे। शौकिया लेखन और गम्भीर साहित्य के फर्क़ को समझना नितांत आवश्यक बन पड़ा है।
इन सब बातों का उद्देश्य लेखन/लेखक को निराश करना नहीं बल्कि उसमें एक नई सोच उत्पन्न करना है जो मौलिक हो। उसकी रगों में विश्वास भरना है कि उसकी लेखनी को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं वोअपने शब्दों से कितनों को आस दे सकता है। उसके ह्रदय में साहस उत्पन्न करना है जो इन पथरीली राहों पर किसी के साथ की उम्मीद किये बिना निडर हो चल सकता है।
हमें दुनिया को यह दिखाना है कि कलम हमारी ताक़त है, कमजोरी नहीं!
किताबें सिर्फ़ किताबें नहीं,
एक अनुभव है, उम्र है, जीवन है
और जीवन की ही तरह इसमें सुख है तो दुःख भी
कुछ हंसी ख़यालात, कुछ सपने,
थोड़ी मायूसी, थोड़ी ख़ुशी,
थोड़ा इंतज़ार, थोड़ी तक़रार,
दर्शन, ज्ञान, शिक्षा की बातें हैं।
कभी करती है ये घुमक्कड़ी, तो कभी
पैर पसारे फैल जाती हैं रेत पर
हर समय, हर मूड, हर विषय पर
मिल जायेंगी तुम्हें किताबें
रखो इन्हें तकिए के नीचे
या कभी तकिया ही बनाकर सो जाओ
बचपन की यादों की तरह
ये भी तो सोई हैं कितनी दफे
हमारे ही सीने पर सर रख
तो कभी उलटे पड़े मेढक की तरह
तकती हैं राहें कि आये कोई,
लगा ले गले इन्हें!
हमसफ़र, अपनी-सी,
कभी हंसाती, कभी रुलातीं,
कभी बदल देतीं जीवन-दिशा ही
अब ये हम पर है कि हम क्या पढ़ें
क्योंकि हर मोटी ज़िल्द के अंदर भरे
पन्नों की फड़फड़ाहट
‘क़िताब’ नहीं होती
‘साहित्य’ अत्यंत आदरणीय शब्द है
लिखना आसान है, शायद छपना भी
पर साहित्य को पढ़ने और समझने के लिए
मीलों दूर चलना, शेष है अभी……!
किताबें हैं….रहेंगीं, तुम्हारे जाने के बाद भी और मनुष्य की आखिरी सभ्यता तक।
– प्रीति अज्ञात